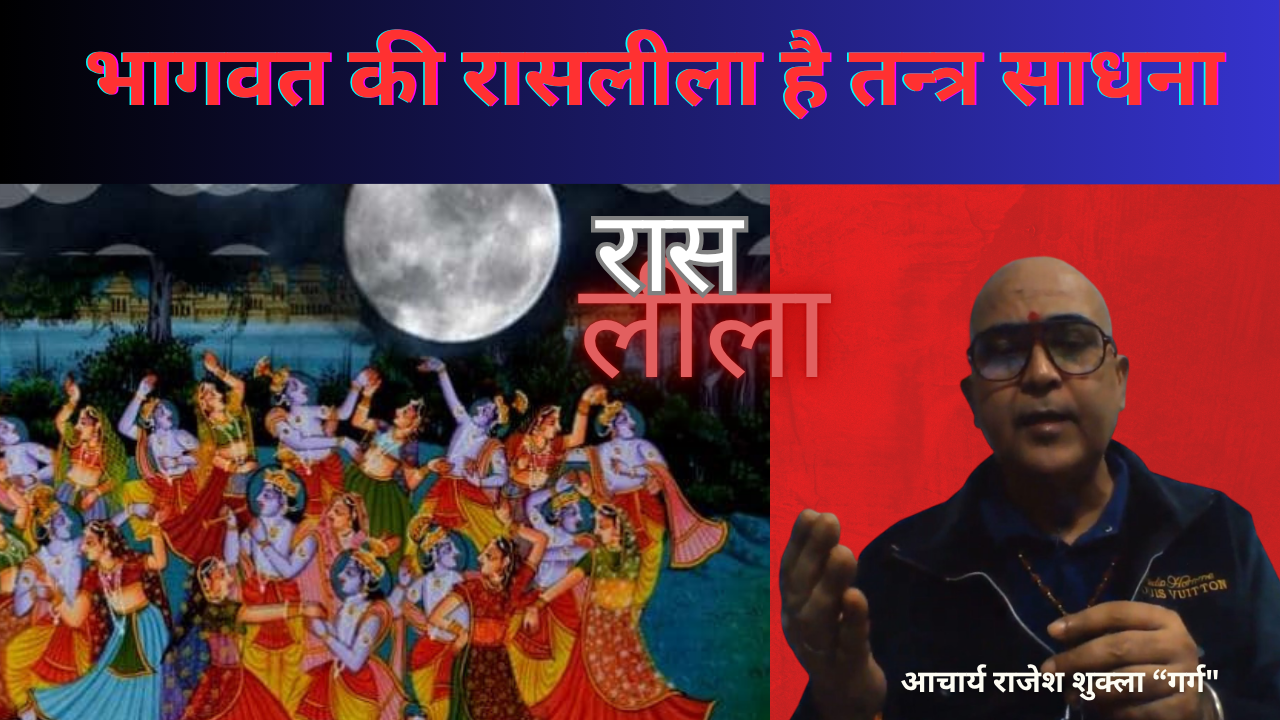भारत के मन्दिरों में किसी गुरु की पूजा नहीं होती. उन मन्दिरों को छोडकर जिसे आधुनिक सम्प्रदाय के धूर्त बाबाओं ने बनाये. ऋषियों और आचार्यों ने मन्दिर में गुरु पूजा का प्रावधान कभी नहीं किया, आदि’ शंकराचार्य ने कितने ही मन्दिरों की स्थापना और उद्धार किया लेकिन अपना मन्दिर उन्होंने नहीं बनाया? वर्तमान समय में किसी के भीतर भी गुरु तत्व नहीं है लेकिन खुद को पूजवाने की लालसा बहुत है. इस लालासा के होने के कारण भगवान का मन्दिर बनाकर स्वयं का भी मन्दिर बना लेते हैं. जो बलात्कारी बाबा हुए आशाराम बापू की तरह उन्होंने भी अपने मन्दिर बना लिए थे. इनमें ज्यादातर तो प्रवचन करने वाले धूर्त हैं जिनको बड़ी मात्रा में काला धन प्राप्त हुआ. ये गुरु नहीं थे, पौराणिक धूर्त थे. इन्होने धर्म की वृद्धि नहीं की अधर्म की वृद्धि की. समाज में जब धर्म की वृद्धि होती है तो समाज में सुख-शांति आती है. जनता का ऐश्वर्य बढ़ता है. इन अधर्मी बाबाओं के कारण समाज में लूटपाट, बलात्कार, ठगी अपने चरम पर है. कार्य-कारण के सिद्धांत से यही सिद्ध होता है कि इसके होने से यह होता है, इसके होने से यह नहीं होता. धर्म की वृद्धि होने से समाज में अधर्म और अनाचार कम हो जाता है जबकि इसके विपरीत ही देखने में आ रहा है. इससे सिद्ध है कि मूलभूत रूप से अधर्म की प्रेक्टिस की जा रही है.
आध्यात्मिक जगत के गुरुओं के भीतर कुछ न कुछ ईश्वर का प्रकाश रहता है क्योंकि वह शुद्ध, मुक्त, आत्माराम होते हैं. इन गुरुओं में सम्प्रदायिक चेतना नहीं होती. गुरुओं में कई कटेगरी बना सकते हैं चेतना के विकास के अनुसार. कुछ लौकिक गुरु होते हैं, कुछ धर्म जगत में पुराण-पुजारी टाईप के होते हैं जिनमे ज्ञान का प्रकाश नहीं होता और जातिवाद जैसी रूढ़ियों को धर्म के अंतर्गत मानते हैं और धर्म का बिजनेस करते हैं. इनसे ऊपर आदि शंकराचार्य जैसे गुरु होते हैं जिनकी चेतना बहुत उन्नत होती है, उनमें ईश्वरीय प्रकाश रहता है परन्तु उनमें भी पूर्णता नहीं होती. इनसे ऊपर ईश्वर कोटि के गुरु होते हैं. ये गुरु ऋषियों के अवतार होते हैं. ये हजार दो हजार साल में पैदा होते हैं. इन गुरुओं द्वारा ही ईश्वर संसार को ज्ञान प्रदान करता है. गुरु ईश्वर का मुख है. उस ईश्वर ने ही अनेकों मार्ग बनाये, अनेकों सम्प्रदाय बनाये ताकि अपनी रूचि और स्वभाव के अनुसार मनुष्य उनकी खोज करे. उन सभी गुरुओं में किंचित ईश्वर का प्रकाश था जिन्होंने सांख्य, योग, पाशुपत इत्यादि पन्थ और सम्प्रदाय बनाये, लेकिन उसमें कोई भी पूर्ण नहीं था इसलिए अनेकानेक मतों के बाद भी मत बनते ही गये. मनुष्य पूर्णता प्राप्ति के लिए प्रस्थान करता गया . महिम्न स्तोत्र में कहा गया है –
त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च ।
रुचिनां वैचित्र्याद्ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥
त्रयी, सांख्य, योग, पाशुपत मत और वैष्णव मत, इत्यादि इन भिन्न, भिन्न प्रस्थानों में से रुचि की विचित्रता के अनुसार कोई एक को श्रेष्ठ और अन्य को कनिष्ठ मत कहेगा ! परन्तु सरल, अथवा टेढे मार्ग से जानेवाली सभी नदियाँ, जैसे अंत में समुद्र में जा मिलती है. वैसे ही रुचि वैचित्र्य से भिन्न भिन्न मार्गो का अनुसरण करनेवाले, सभी का अंतिम स्थान हे शिव, आप ही हैं.
सनातन धर्म में प्रस्थान क्यों हैं? वेद के कर्मकांड परक ज्ञान से ऋषियों का पहला प्रस्थान उपनिषद है- जिसे वेदांत कहते हैं. यह वेदों का शीर्ष भाग है. एक अद्भुत ईश्वरीय प्रज्ञा द्वारा भारत के अनेकानेक वेद विरोधी दर्शनों और मतों का निषेध कर, उपनिषदों के ज्ञान को एकसूत्र में पिरोने वाले भगवान बादरायण ने दूसरे प्रस्थान का मार्ग प्रशस्त किया, फिर पराशर और उनके पुत्र वेदव्यास तथा शुकदेव ने श्री कृष्ण के माध्यम से भगवद्गीता उपदेश द्वारा तीसरे प्रस्थान को जन्म दिया. तीसरे प्रस्थान में वैदिक-सांख्य-योग-पौराणिक मत सभी को एकसूत्र में पिरोया गया. यह प्रस्थान सभी को समाहित करने वाला हो गया. यह प्रस्थान भी अंतिम नहीं है. समय के अनुसार यहाँ से प्रस्थान करना होगा. भगवद्गीता के बाद सांख्य दर्शन एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में खत्म हो गया जबकि वही सांख्य बादरायण के ब्रह्मसूत्र में प्रमुख प्रतिपक्षी है. भगवद्गीता और भागवत के बाद गौतम बुद्ध का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह गया, वे विष्णु के अवतार हो गये. गौरतलब है कि भारत से बौध धर्म का पूर्णत: उच्छेद करने वाले आदि शंकराचार्य ने ही भगवद्गीता पर पहला भाष्य लिखा था.
यह सिर्फ आध्यात्मिक जगत की ही बात नहीं है. यह प्रस्थान मनुष्य की प्रकृति में निहित है. राजतन्त्र से प्रस्थान कर मनुष्य जनतन्त्र तक आया. राजतन्त्र को मानने वाले ही बाद में फासिस्ट हो गये जो एक नेता-एक-पार्टी और एक वर्ग के शासन में विश्वास करते हैं और दमन के हिमायती हैं. दुनिया के तमाम बड़े वैज्ञानिकों, दार्शनिको और चिंतकों में भी ईश्वरीय चेतना काम करती है. ईश्वर ही युगानुकुल उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रकट कर कुछ नई सोच, नये विचार, कोई नया अविष्कार करने की प्रेरणा देते हैं और ज्ञान के क्षेत्रों में नई क्रांतियाँ होती हैं जिससे मनुष्यता का कल्याण होता है. धर्म के गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति से मनुष्यों का कल्याण करते हैं इसलिए सनातन धर्म में गुरु ईश्वर जैसा कहा गया है. गुरु को ईश्वर के समकक्ष स्थापित करने वाले लोग प्रमुख रूप से पतंजली के सूत्र को ही आधार मानते हैं – “क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर: !” वह पुरुष विशेष जो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से रहित है वह ईश्वर जैसा है. ईश्वर की यह परिभाषा सांख्य दर्शन की परिभाषा है जिसे सभी गुरु अपने लिए प्रयोग करने लगे और खुद को पूजवाने लगे…लेकिन वेदांत में ईश्वर रचनाकर्ता, पालनहार और संहारकर्ता भी है. उसने ब्रह्मा को भी सृष्टि के लिए वेदों का ज्ञान प्रदान किया, उन्होंने ही प्रकृतिलयों को भी योग का ज्ञान प्रदान किया. ईश्वर त्रिकालाबाधित सत्य है, काल उसका अवच्छेदन नहीं करता, वह आदि गुरु है “स एष पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात् ” सबसे पहले ब्रह्मा को उसने ही ज्ञान प्रदान किया. वेदव्यास यही लिखते हैं –
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्।
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः ।।
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ।।
यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि सांख्य में ईश्वर का सिद्धांत बाद में जोड़ा गया, प्रारम्भिक सांख्य जिसका उपदेश कपिल ने किया था उसमे पुरुष और प्रकृति के इतर कोई दूसरा तत्व नहीं था.
पतंजली के दर्शन में भी जिसको गुरु कहा गया है, जिसमे सभी श्रुतियों का बीज है अर्थात समस्त ज्ञान का बीज है, वह वेदांत का ही ईश्वर है. संभवत: योगसूत्र के कुछ सूत्र वेदांत के गुरुओं द्वारा बाद में जोड़ा गया था.