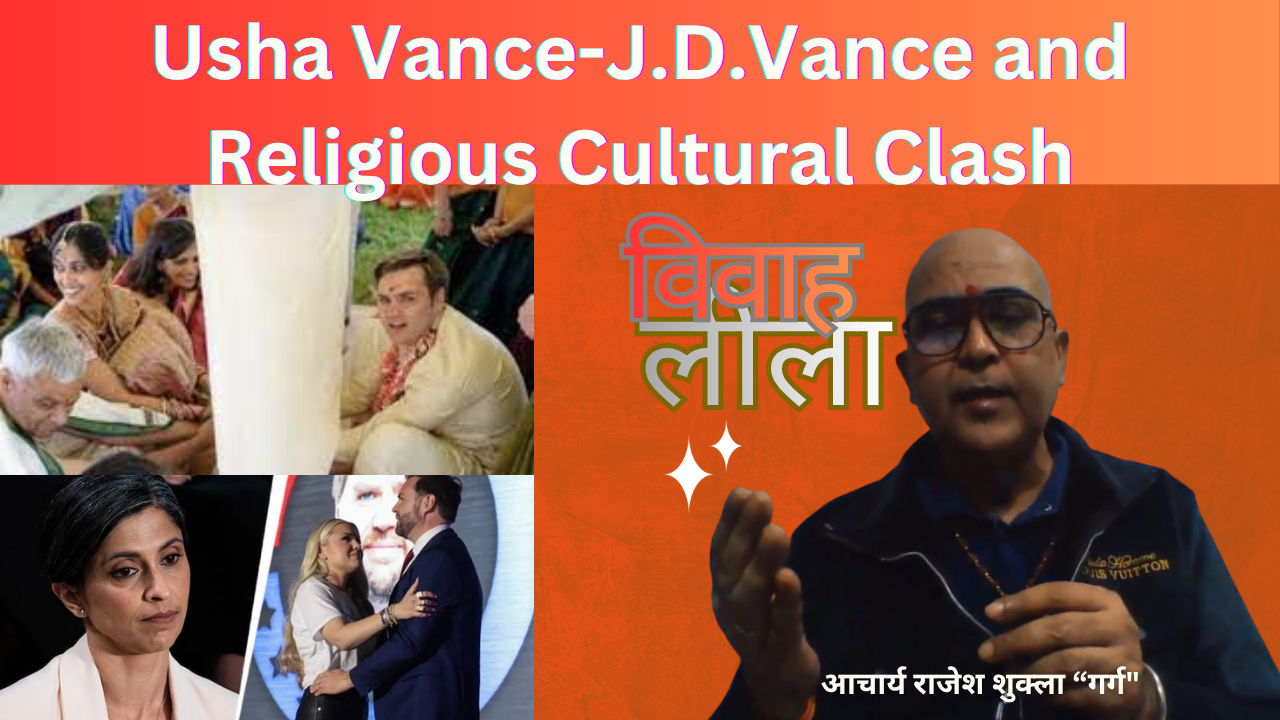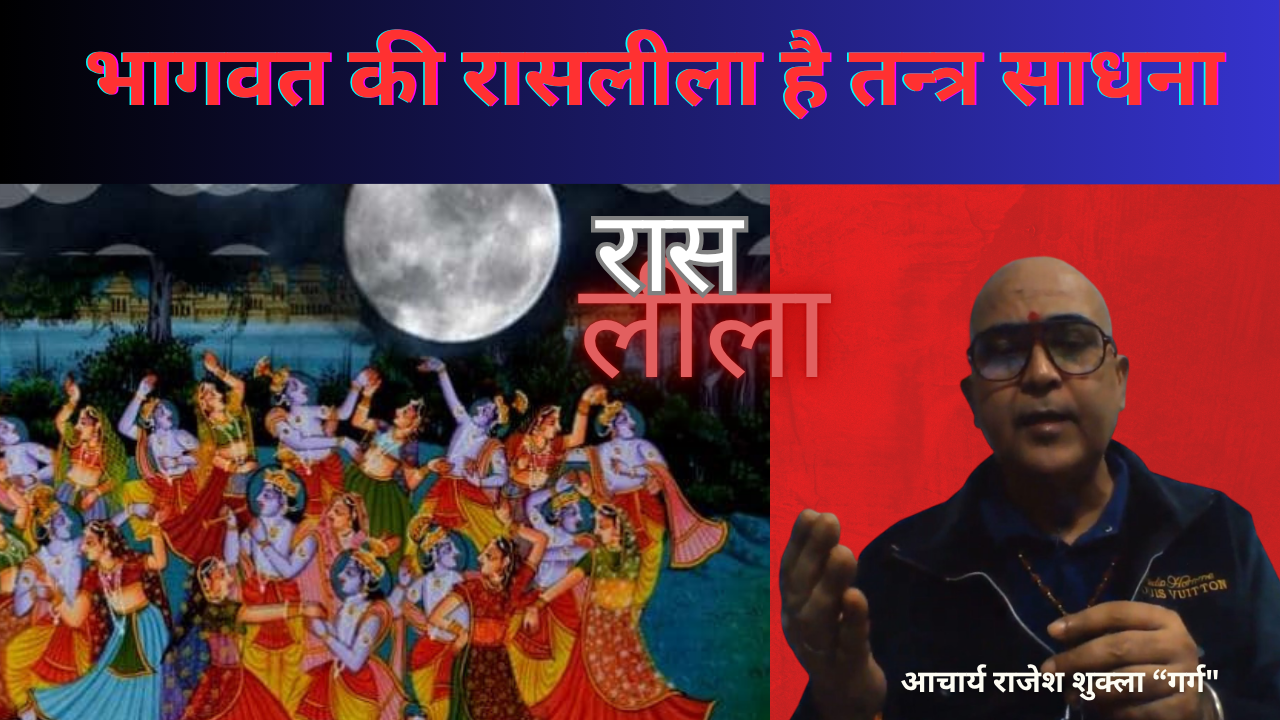अध्यात्म विज्ञान में स्थान-स्थान पर प्रकाश की साधना और प्रकाश की याचना की गई है. “असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय .. यह प्रकाश नहीं वरन् वह परम ज्योति है जो इस विश्व में चेतना का आलोक बनकर जगमगा रही है. गायत्री का उपास्य सविता देवता यह परम ज्योति है. इसका अस्तित्व ऋतम्भरा प्रज्ञा के रूप में प्रत्यक्ष और कण-कण में संव्याप्त जीवन ज्योति के रूप में प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर भी देख सकता है. इसकी जितनी मात्रा जिसके भीतर विद्यमान हो समझना चाहिए कि उसमें उतना ही अधिक ईश्वरीय अंश आलोकित हो रहा है.
गायत्री उपासना में सविता देवता का ध्यान करने की प्रक्रिया इसीलिए की जाती है कि अन्तर के कण-कण में संव्याप्त प्रकाश आभा को अधिक दीप्तिमान बनने का अवसर मिले. अपने ब्रह्म रंध्र में अवस्थित सहस्राँशु-आदित्य सहस्रदल कमल को खिलाये और उसकी प्रत्येक पंखुड़ी में सन्निहित दिव्य कलाओं के उदय का लाभ साधक को मिले.
ब्रह्म विद्या का उद्गाता ‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ की प्रार्थना में इस दिव्य प्रकाश की याचना करता है. इसी की प्रत्येक जाग्रत आत्मा को आवश्यकता अनुभव होती है, इसलिए गायत्री उपासक अपने जप प्रयोजन में इसी ज्योति को अन्तः भूमिका में अवतरण करने के लिए सविता देवता का ध्यान करता है. उसे पवित्रता, मेधा, प्रखर प्रतिभा मिले.
“वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके बताया है कि नक्षत्रीय गतिविधियाँ मनुष्य की मानसिक व शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं. एक वैज्ञानिक प्रयोग में यह बात सामने आई कि मनुष्य की कोशिकाओं में अनुकूल तत्वों को आकर्षित करने, अवशोषण कर अपने में धारण करने और इस आधार पर शरीर से टूटने वाली ऊर्जा की कमी को पूरा करने की अद्भुत सामर्थ्य है. इसकी जाँच हुई और जब शरीर के जीवित अंश को काट कर अलग रखा गया उस स्थान पर पहले से एक विषाक्त रसायन रखा था मस्तिष्कीय प्रक्रिया से सम्बन्ध विच्छेद होने पर भी उस जीवित टुकड़े के अणु उस घातक वस्तु से दूर हटने की कोशिश करने लगे. तुरंत उस विष को वहाँ से हटा दिया और उस स्थान पर लाभदायक औषधि रखी तो उन कोषाणुओं का गुण पूरी तरह बदल गया वे उस औषधि की ओर खिंचने का गुण दिखाने लगे.
इसी आधार पर मनुष्य आकाश की दृश्य- अदृश्य शक्तियों से तो प्रभावित होता ही है मन की चुम्बकीय शक्ति प्रवाह भी अपने अन्दर आकर्षित कर धारण कर सकता और अपनी अन्तरंग क्षमताओं को विकसित कर सकता है. प्राचीन भारतीय मनीषियों ने इन्हीं शक्ति प्रवाहों को सूक्ष्म दैवी शक्तियों के रूप में माना था, उनके गुणों की पृथकता के आधार पर उन्हें पृथक्- पृथक् देव शक्तियों की संज्ञा देकर उनकी उपासना की विधियाँ विकसित की थीं और उनके प्रचुर भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष उपलब्ध किया था. क्वांटम थ्योरी ने परिपूरक सिद्धान्त के रूप में यह स्वीकार किया है कि पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से तरल, तरल से गैस, गैस से प्लाज्मा तथा इसी तरह के और भी उन्नत किस्म के प्रकाश-कणों में परिवर्तित हो जाता है उसी तरह उच्चस्तरीय चेतन कण क्रमशः एक स्थिति में पदार्थ के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं. इसी तरह का प्रतिपादन वैज्ञानिक हाइज़ेनबर्ग ने भी किया और लिखा है कि अन्तरिक्ष में एक स्थान आता है जहाँ पदार्थ को छोड़ दिया जाये तो वह स्वतः ऊर्जा में परिणत हो जाता है जिस तरह पदार्थ सत्ता परिधि काल और रूप के ढाँचे में बंधी रहती है उसी तरह मनःसत्ता अनुभूति-स्मृति, विचार और बिंब के रूप में व्यक्त होती है इतना होने पर भी दोनों में अत्यधिक घनिष्ठता है. यह एक दूसरे को प्रभावित ही नहीं करते अपितु परस्पर आत्मसात भी होते रहते हैं. सविता ध्यान का अर्थ इस प्रक्रिया को ही प्रगाढ़ बनाकर उन शक्तियों से लाभान्वित होना है.
सविता देवता यद्यपि सूर्य का ही दूसरा नाम है. पर यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जो अन्तर शरीर और आत्मा का है वही सूर्य और सविता का है. गायत्री महामन्त्र का देवता सूर्य वही महाप्राण है. उसका स्पष्टीकरण शास्त्रों में स्थान-स्थान पर विस्तारपूर्वक किया गया है.
योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽहम् (मैत्रेयी उपनिषद् 6/35)
अर्थात्-(जो सूर्य है सो मैं हूँ )।
सूर्य के माध्यम से प्रस्फुटित होने वाला महाप्राण परब्रह्म परमात्मा का वह अंश है जिससे इस विश्व-ब्रह्मांड का संचालन होता है. एक से अनेक बनने का ब्रह्म-संकल्प ही महाप्राण बन कर फूट पड़ा है. यह निर्झर जिस दिन तक झर रहा है. उसी दिन तक सृष्टि है. जिस दिन परम प्रभु उस संकल्प को समेट लेंगे उसी दिन महाप्राण शाँत हो जायेगा और फिर महाशून्य के अतिरिक्त और कुछ भी शेष न रहेगा. यह ब्रह्मसंकल्प-महाप्राण-परब्रह्म की सत्ता से भिन्न कोई बाहरी पदार्थ नहीं वरन् उसी का एक अविच्छिन्न अंग है. परमात्मा अनन्त है उसकी सत्ता असीम है. उस अनन्त, असीम, अचिन्त्य का एक भाग जो सृष्टि के संचालन में, उनकी समस्त प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित रखने में लगा हुआ है, उस महाप्राण को ही सूर्य की आत्मा-सविता देवता समझना चाहिए. प्राणी का, जीवधारी का सीधा सम्बन्ध इसी से है.
यह महाप्राण जब शरीर क्षेत्र में अवतीर्ण होता है तो आरोग्य, आयुष्य, तेज, ओज, बल, उत्साह, स्फूर्ति, पुरुषार्थ, इन्द्रिय शक्ति के रूप में दृष्टिगोचर होता है जब वह मनःक्षेत्र में अवतीर्ण होता है तो उत्साह, स्फूर्ति, प्रफुल्लता, साहस, एकाग्रता, स्थिरता, धैर्य, संयम आदि सद्गुणों के रूप में आता है. जब उसका अवतरण आध्यात्मिक क्षेत्र में होता है तो दैवी गुणों त्याग, तप, श्रद्धा-विश्वास, दया, उपकार, प्रेम, विवेक आदि के रूप में दिखाई देता है. तीनों ही क्षेत्र उस महाप्राण में जैसे-जैसे भरते जाते हैं वैसे ही मनुष्य अपूर्णता से पूर्णता की ओर, लघुता से विभुता की ओर, तुच्छता से महानता की ओर बढ़ने लगता है. आत्म कल्याण का, लक्ष्य प्राप्ति का यही मार्ग है. गायत्री के द्वारा सविता देवता को-महाप्राण को उपलब्ध करने का प्रयोजन ही यही है. शतपथ ब्राह्मण का ऋषि कहता है-
“यौ वे प्राण सा गायत्री “ (शत. 1/3/5/15)
“जो प्राण है, उसे ही निश्चित रूप से गायत्री जानना” ।
गायत्री का देवता सविता अर्थात् गायत्री उपासना के समय सूर्य के ध्यान की व्यवस्था है उसका अर्थ सूर्य की अदृश्य शक्तियों, किरणों को उपरोक्त वैज्ञानिक, सिद्धान्तों के आधार पर शरीर में धारण करना और उसके आत्मिक व वैज्ञानिक लाभों से लाभान्वित होना है. हमारी प्रगाढ़तम ध्यानावस्था हमारी मनश्चेतना को “ सूर्य” बना देती है इसलिए “सूर्य आत्मा” यह वेद मन्त्र है.
वैज्ञानिक प्रयोग ज्योतिष सिद्धांत की ताकीद करते हैं कि ग्रहों के कुप्रभाव से अनुष्ठान द्वारा बचा जा सकता है और अच्छे रत्न भी काफी प्रभावी हो सकते हैं.