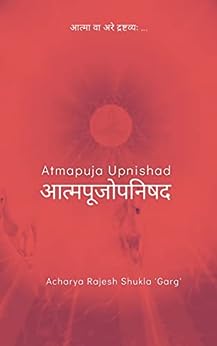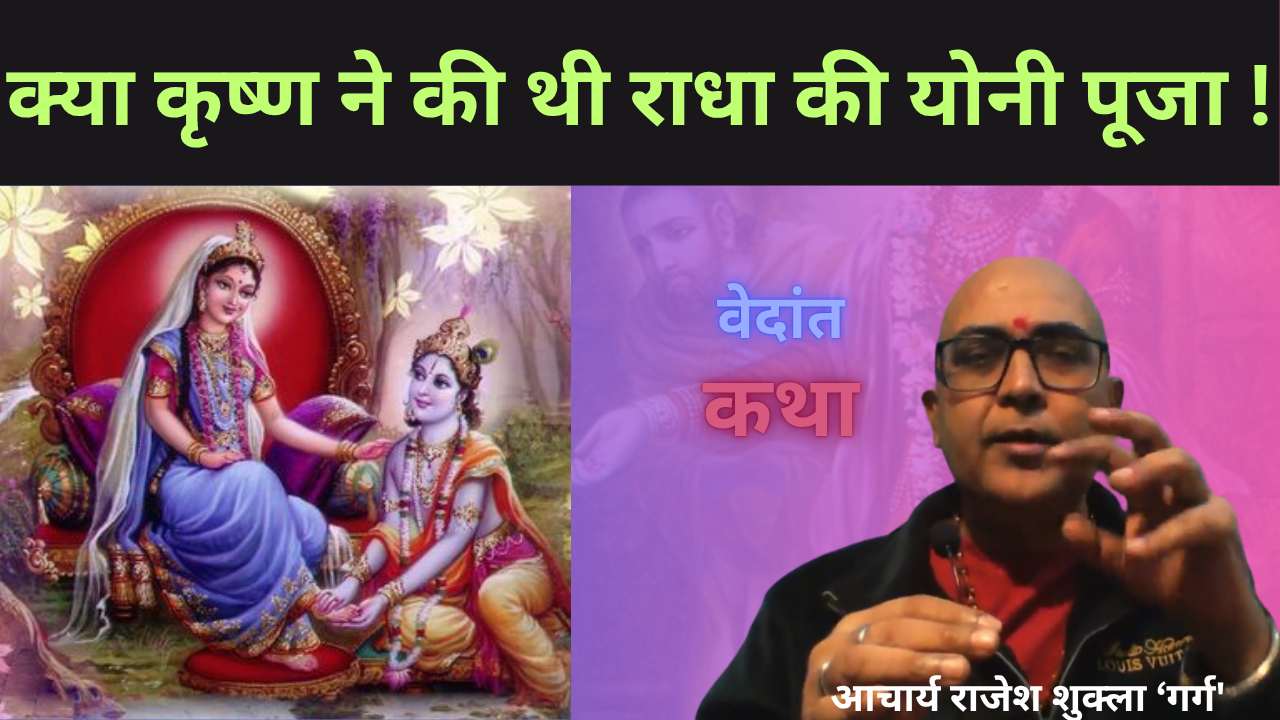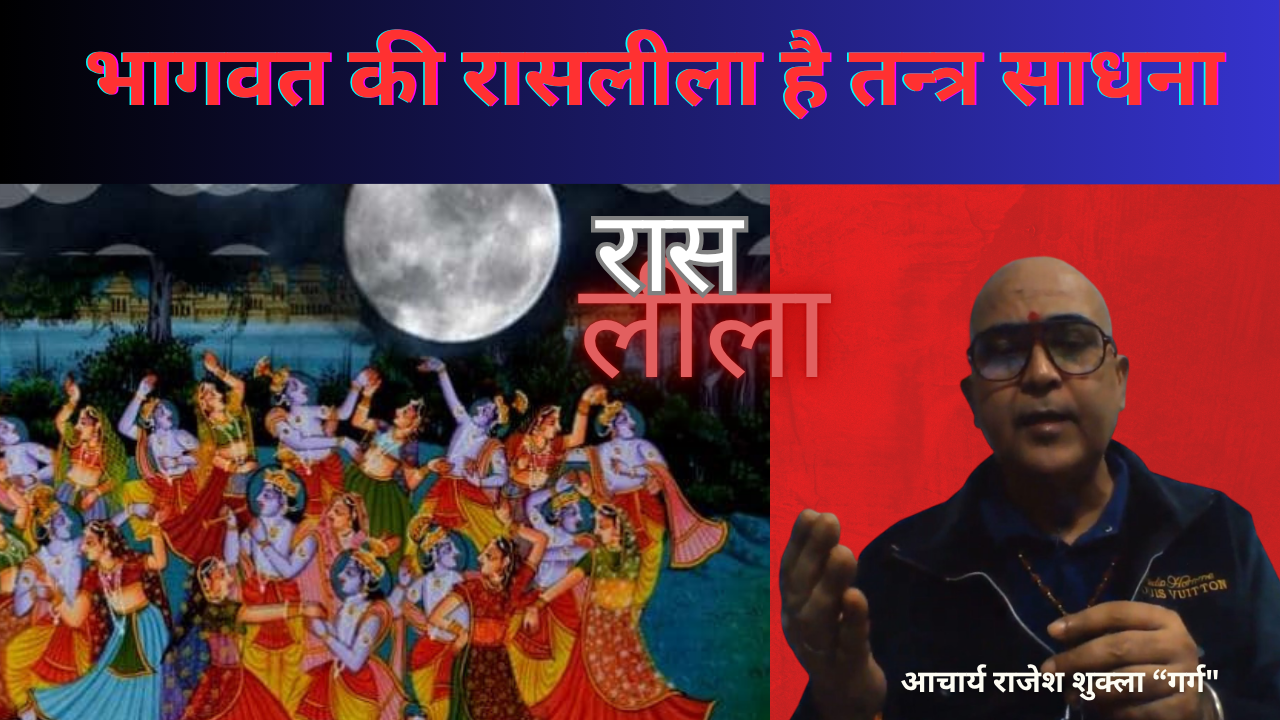सूर्यात्मकत्वं दीप:
सूत्र में प्रकरण आत्म देवता को दीप दिखाने का है। श्रुति कहती है कि उस आत्मतत्व का सूर्यात्मकत्व ही उसके लिए दीप है। कहीं बाहर का दीपक दिखाने की जरूरत नहीं, यह प्रकाश तो उस आत्मा का निज स्वरूप ही है। आत्मा और उसका सूर्यात्मकत्व यह एक गूढ़ विषय है। ब्रह्मविद्या शास्त्रों में इस विषय को बहुत विस्तार से बताया गया है लेकिन क्योंकि वेदांत गुरुगम्य विद्या है इसलिए इसकी समझ बिरले लोगों को ही हो पाती है। आत्म तत्व का सूर्यात्मकत्व यह जो प्राकृत सूर्य प्रकाशित होता उससे नहीं है बल्कि उस सूर्य से है जो सूर्यो का भी सूर्य है, ज्योतियों का भी ज्योति है। आत्मतत्व के सूर्यात्मकत्व को प्रभाषित करती यह छान्दोग्य श्रुति प्राप्त होती है –
आदित्प्रत्नस्य रेतस उद्वयं तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तर स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति॥
ब्रह्म जो प्रकाशों का प्रकाश हैं, जो सर्वव्यापी है , जो अज्ञान का विनाशक है उस प्रकाश को अपने आत्मतत्व से अलग न देखते हुए हम सूर्यात्मकत्व को प्राप्त हुए अर्थात समस्त देवताओं में देव सूर्य को प्राप्त हुए जो सभी प्राणियों के प्रेरक हैं। अनेक श्रुतियां हैं जिनमें आत्मा के सूर्यात्मकत्व के बारे में अलग अलग तरीके से कहा गया है।
बृहदारण्यक श्रुति के अनुसार -आत्मैव अस्य ज्योतिर्भवतीति, आत्मनैव अयं ज्योतिषा आस्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीति । अधिभौतिक सूर्य इत्यादि के अस्त होने के बाद यह आत्मा अपने प्रकाश से ही समस्त क्रियाओं को करता है।
योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः ….ध्यायतीव लेलायतीव । – बृहदारण्यकोपनिषत् ४-३-७
यह जो विज्ञानंमय ज्योतिःस्वरूप वाला पुरुष है वह इस लोक और मृत्युलोक का अतिक्रमण करता है। यह पुरुष सर्वगत है, पूर्ण है, यह सबका प्रकाशक है इसलिए इसकी स्वयंप्रकाशता सबसे बढ़ कर है।
छान्दोग्य श्रुति में इस परम ज्योति को ही आत्मा में प्रकाशित ज्योति कहा गया है, यथा-
अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः तस्यैषा दृष्टिर्यत्रितदस्मिञ्छरीरे सस्पर्शेनोष्णिमानं विजानाति तस्यैषा श्रुतिर्यत्रैतत्कर्णावपिगृह्य निनदमिव नदथुरिवाग्नेरिव ज्वलत उपशृणोति तदेतद्दृष्टं च श्रुतं चेत्युपासीत चक्षुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद य एवं वेद॥
सूर्य का प्रकाश अन्तरिक्षलोक से ऊपर नहीं जाता अतएव यह सबका प्रकाशक अन्तर्यामी नहीं हो सकता है इसलिए श्रुति कहती है -इस द्यौ लोक से परे जो परम ज्योति विश्व के पृष्ठ पर यानि सबके ऊपर, जिनसे उत्तम दूसरा कोई लोक नहीं है, ऐसे उत्तम लोको में प्रकाशित हो रही है; वह निश्चय ही यही है जो कि इस पुरुष के भीतर ज्योति है।
गायत्री महाविद्या भी आत्मा और उसके सूर्यात्मकत्व को ही प्रकट करती है लेकिन गायत्र ब्रह्म परब्रह्म नहीं है, हो भी नहीं सकता क्योंकि अक्षर रचना रूप गायत्री सर्वात्मक नहीं हो सकती। इस सन्दर्भ को छान्दोग्य में स्पष्ट करते हुए ऋषि ने निर्देशित भी किया है कि यह जो कुछ भी है वह गायत्री ही है, इसका एक पाद ही सम्पूर्ण लोक हैं तीन पाद तो अमृतमय लोकों में स्थित हैं। गायत्री का चतुष्पादत्व ब्रह्म के अनुगत होने से ही है क्योंकि भूतादि छंद के पाद नहीं हो सकते। छान्दोग्य श्रुति में ऋषि ने ‘वाग्वा इदं सर्व भूतं’ द्वारा इसे स्पष्ट किया है। उपनिषद में यह गायत्री ब्रह्म की तरह ही चार पादों वाली है, यह बता कर कहा गया है कि इस गायत्री संज्ञक ब्रह्म की महिमा इतनी ही है-
तावानस्य महिमा ततो ज्यायाश्च पूरुषः।
पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीति॥
इस गायत्र्य ब्रह्म में अनुगत जो पुरुष है वही उत्कृष्ट है, वही ज्योतियों का ज्योति है। ब्रह्मसूत्र के ‘ज्योतिश्चरणाभिधानात्’ के भाष्य में आदि शंकराचार्य ने इस विषय को विस्तार से समझाया है। जिस प्रकार से गायत्री में अनुगत ब्रह्म को ही ज्योति कहा गया है, उसी प्रकार प्रणव, सूर्य और प्राण की एकता बतलाने वाली श्रुतियों का अर्थ समझना चाहिए है –
अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ इत्यसौ वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणव ओमिति ह्येष स्वरन्नेति॥
यह जो चक्षु स्थित पुरुष है और जो आदित्यान्तर्गत पुरुष है, ये दोनों एक ही हैं; यह जो प्राण संज्ञक ब्रह्म है और आदित्य संज्ञक ब्रह्म है दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों में एक ही ब्रह्म अनुगत है। यह ब्रह्म सर्व है, यह सबको अतिक्रमण कर स्थित है ‘विश्वतः पृष्ठेषु’।
उपनिषद का यह सूत्र आत्मा के उसी सूर्यात्मकत्व की बात करता है जो सबका प्रकाश है ‘येन सूर्यस्तपति तेजसेद्ध:’ । भगवान ने जब अपने ब्रह्म स्वरूप को प्रकट किया तो उसका प्रकाश सहस्रों सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा था –
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता।
यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः।।
सहस्र सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश होगा, वह उस (विश्वरूप) परमात्मा के प्रकाश के सदृश होगा। वह प्रकाश उस महात्मन् – विश्वरूपके प्रकाशके सदृश कदाचित् हो तो हो? अथवा सम्भव है कि न भी हो अर्थात् उससे भी विश्वरूपका प्रकाश ही अधिक हो सकता है।
इसीप्रकार से आत्मतत्व के सूर्यात्मकत्व की उपलब्धि है जिसे दीप कहा है । इस परम ज्योति के सम्बन्ध में निम्नलिखित श्रुति भी है –
सोऽहमर्कः परं ज्योतिरर्कज्योतिरहं शिवः ।
आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिरसावदोम् ।।
जो इस आत्मा के सूर्यात्मकत्व को जानता है वह काल का अतिक्रमण कर जाता है, उसके लिए सूर्य कभी अस्त नहीं होता ।
मेरी किताब “आत्म पूजा उपनिषद” से साभार –