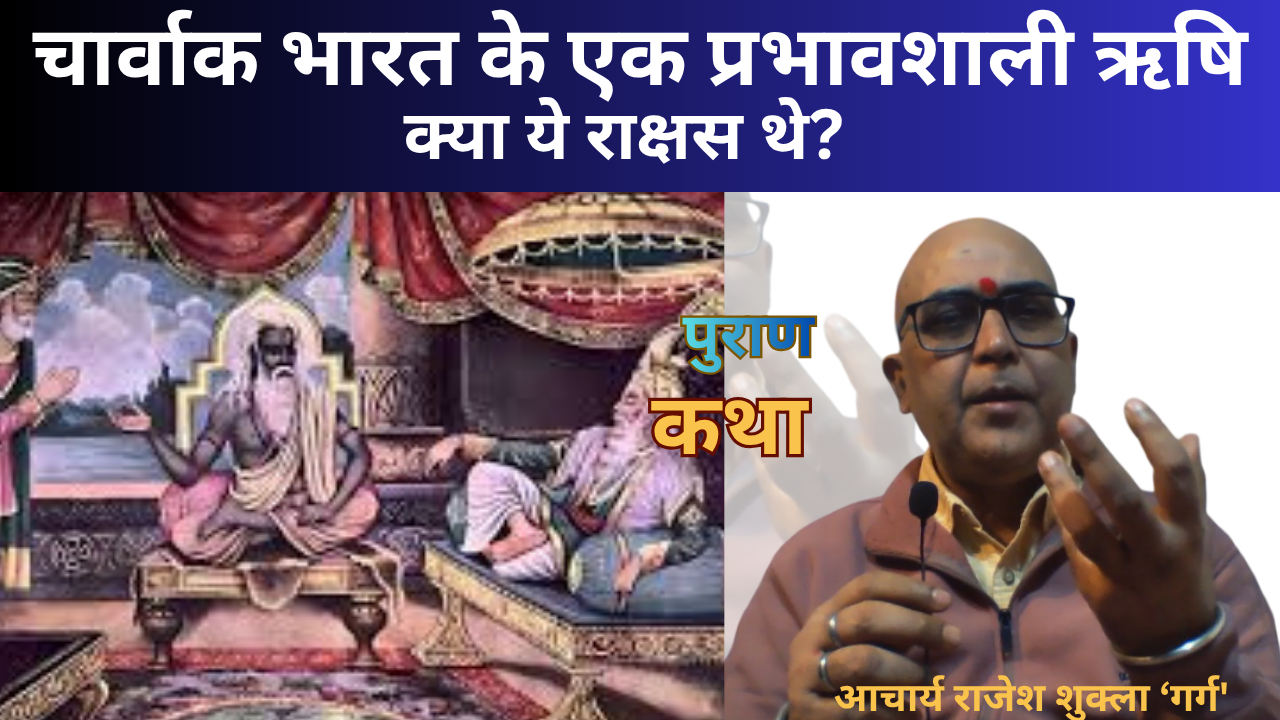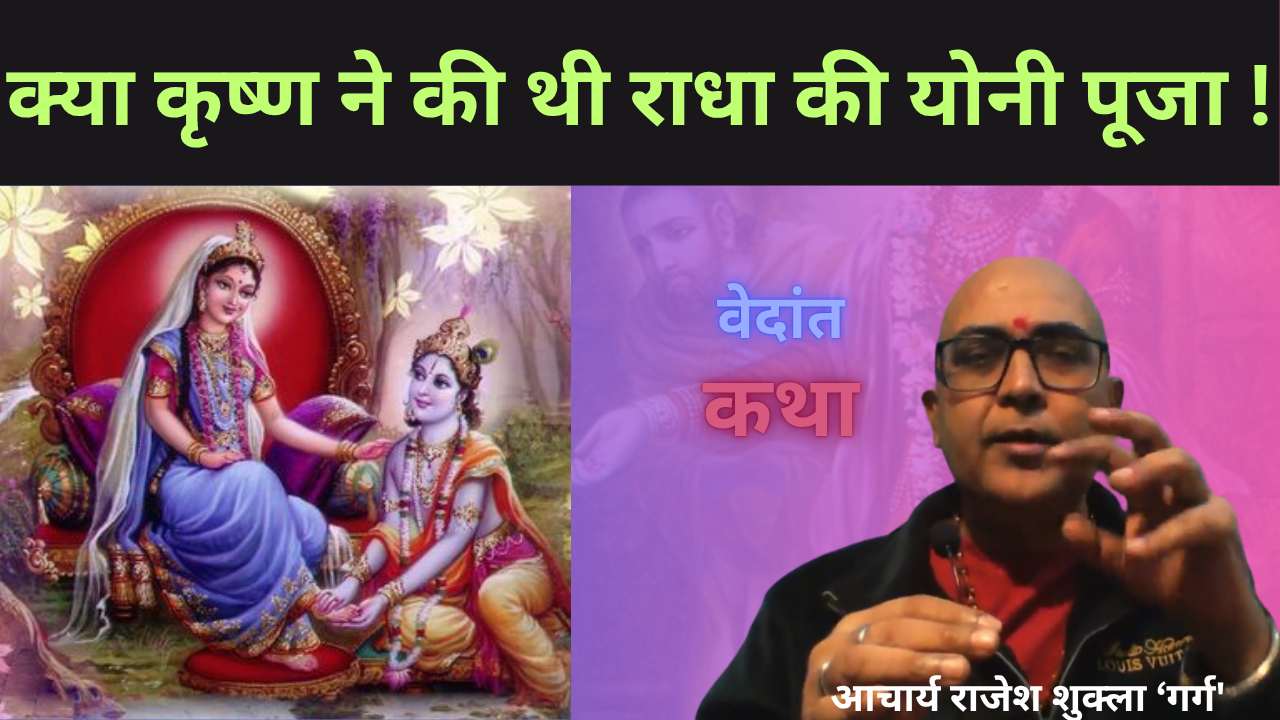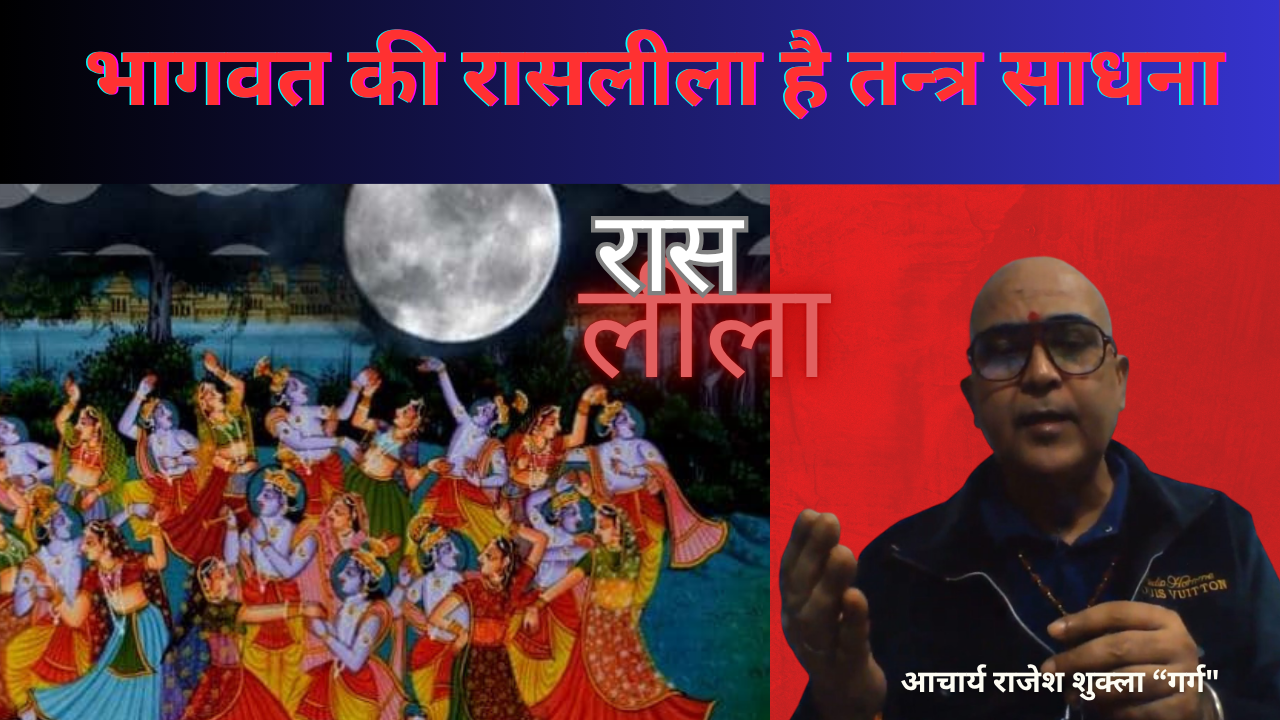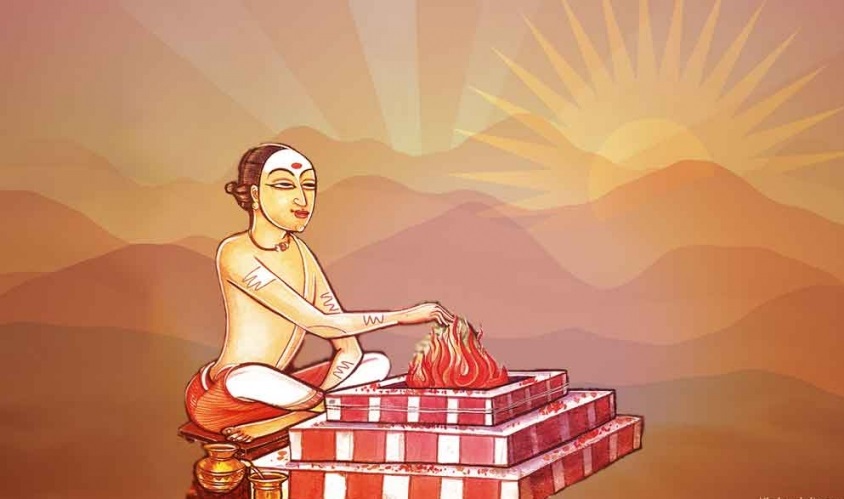
उपनिषदिक आध्यात्म के उच्चतम आयाम में जो कुछ भी कहा गया है वह सब आनंद की मीमांसा है. मन्त्र इस मीमांसा का एक सूक्ष्म आयाम है. मन्त्र शास्त्र में स्तुति और मन्त्र में अंतर किया गया है. मन्त्र, स्तुति, कथा ये तीनों ही विकल्पात्मक हैं, यह समझना चाहिए. अब ये विकल्प किस तरह के हैं? उदाहरण के लिए सिनेमा का एक गीत है ‘मन तड़पत हरि दर्शन को आज मोरे तुम बिन बिगड़े सकल काज” और दूसरा “तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ वफ़ा कर रहा हूँ वफ़ा चाहता हूँ ” दोनों ही अलग अलग तरह से विकल्पात्मक हैं और दोनों से चेतना में अलग अलग ठंग से क्षोभ होता है. पहला गीत सात्विक वासनात्मक है, दूसरे में राजसिक वासना है. इन दोनों विकल्पात्मक गीतों से दो तरह की सिद्धि प्राप्त हो सकती है. पहले से ईश्वर के प्रति थोड़ा प्रेम बन सकता है, दूसरे से कोई लड़की से मोहब्बत हो सकती है. इसी तरह स्तुति देवताओं की महिमा का गायन है जिसके कई प्रकार हैं. कुछ स्तुतियाँ सिर्फ महिमा का गायन करती हैं, कुछ स्तुतियाँ देवता के स्वरूप का वर्णन करने वाली होती हैं, कुछ स्तुतियाँ काफी दार्शनिक चरित्र रखती हैं और कुछ किसी विशेष कामना के लिए गाई जाती हैं. वेदों की ऋचाएं स्तुतियाँ ही हैं, कुछ ईच्छा की प्राप्ति के लिए कही गई हैं और कुछ ईश्वर के दर्शन की कामना को अभिव्यक्त करती हैं लेकिन फिर भी इन्हें वेद मन्त्र कहा जाता है. इन्हें वेद मन्त्र कहने का तात्पर्य यह है कि यह उदात्त ईश्वरीय भावनाएं हैं. वेदों के सूक्तों में कुछ सूक्त बहुत उदात्त हैं इसलिए वे मंत्रात्मक हैं. इन्हीं उदात्त सूक्तों में गायत्री का प्रकटन हुआ है. जिस तरह वेद मन्त्रों का वाचन किया जाता है, क्या वैसा ही वाचन तुलसी दास की कविताओं का भी नहीं किया जाता?
वेदों में यह एक ऋचा है जिसे मन्त्र कहा जाता है –
“ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् |
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्”
वस्तुत: ऋग्वेद के सप्तम मण्डल में उनसठवाँ सूक्त का एक पद्य है जो एक स्तुति है लेकिन यह वेदों की अन्य स्तुतियों से बहुत उदात्त है. सूक्त का अर्थ होता सूक्ति अर्थात किसी का यह वचन है. वशिष्ठ ने यह मंगल श्लोक कहा जो उन श्लोकों से विशिष्ट है, जिनमें इंद्र से धन प्राप्ति की कामना की गई है. इस वेदमन्त्र के वक्ता वशिष्ठ हैं, उन्होंने परमात्मा से जन्म मृत्यु के बन्धनों से मुक्ति की प्रार्थना की है. यह एक संक्षित स्तुति है. यह विकल्पात्मक ही है लेकिन सात्विक होने से यह कल्याणकारी है. इन सात्विक विकल्पों से स्वात्म संस्कार में मदद मिलती है इसलिए ये मन्त्र मान लिए गये हैं. लेकिन पतंजलि जैसे ऋषियों को स्वात्म संस्कार के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वे अपने बल से संस्कार सम्पन्न हो जाते हैं. त्र्यम्बक मन्त्र एक संक्षिप्त स्तुति है, वहीं महिम्न स्तोत्र या शिव तांडव स्तोत्र एक बृहद स्तुति है. यहाँ विकल्पात्मक चित्त थोड़ा और विस्तार को प्राप्त कर गया है. यहाँ शिव की महिमा का गायन आचार्य पुष्पदंत ने किया है. पुष्पदन्त एक गन्धर्व थे जो सभी गन्धर्वों की तरह ही देवताओं की प्रसंशा में गीतों का गायन करते थे. इस स्तोत्र में उन्होंने शिव की महिमा का गायन किया और उन्होंने ‘नेति नेति’ कहने के बाद जो ईश्वर के स्वरूप का चित्रण किया –
श्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचराः।
चिता-भस्मालेपः स्रगपि नृकरोटी-परिकरः।।
अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं।
तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि।।
वह शैव सम्प्रदाय की सगुण छवि है. पुष्पदंत एक शैवाचार्य थे. लेकिन शैव ये नहीं कह सकते कि ईश्वर कि एकमात्र यही छवि (इमेज) है? पुष्पदंत ने भी नहीं कहा कि उनकी छवि ही ईश्वर है. शिव की छवि आपकी अपनी भी हो सकती है क्योंकि शिव इन छवियों के इतर अन्य उदात्त छवियों में भी उतने ही प्रकट हैं. भगवद्गीता में इसीलिए वेदव्यास ने एक अध्याय दिया है जिसमे भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है. इस विभूतियों में जो जो पृथ्वी लोक में उदात्त है, वह ईश्वर की दिव्य मूर्ति का कुछ संदेश देते हैं. “स्रोतसामस्मि जाह्नवी” नदियों में मेरे छवि को गंगा में दर्शन करो. गंगा नदियों में सबसे उदात्त हैं, सबसे पवित्र हैं लेकिन गंगा परमात्मा नहीं है. यहाँ सवाल यही है कि आपके विकल्पात्मक चित्त में उनकी किस तरह की छवि प्रकट हो सकती है. हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे दार्शनिक कवि हैं तो आपके दर्शन की जितनी उड़ान है उसके अनुसार शिव आपके चित्त में समा जायेंगे. हिन्दू धर्म में षडदर्शनों की पूजा इसीलिए की जाती है “ॐ नमो नारायणाय विष्णुदेवताधिष्ठित वैष्णवदर्शन श्री पादुकां पूजयामि या रूद्रदेवताधिष्ठित शैवदर्शन श्री पादुकां पूजयामि नम: “. मेरे मत के अनुसार आप ईश्वर विरोधी होंगे यदि आप कहते हैं कि षडदर्शनों के बाद विकल्पात्मक चित्त की दार्शनिक उड़ान और कल्पना रुक गई है और अब कोई दूसरा दर्शन होगा ही नहीं . हिन्दू धर्म में सैकड़ों सम्प्रदाय यूँ ही तो नहीं बन गये? यदि हम कहें कि आनंद ही हमारा ईश्वर है और आनंद की कोई छवि नहीं होती, उसका सिर्फ भोग होता है और इस भोग से ही ईश्वर के आनंदमय स्वरूप को जाना जा सकता है. मेरे इस कथन से जितने विकल्पात्मक ईश्वर की छवियाँ हैं उनका सम्हार हो जाता है. क्या नहीं होता !
दर्शन भी मंत्रात्मक ही हैं लेकिन मन्त्र का चरित्र इससे अलग है. ब्रह्म तत्व के चिन्तन या ब्रह्मचर्या (ब्रह्म चरिया) को भी कथा जप कहा गया है. ईश्वर के स्वरूप चिन्तन में कोई बाधा नहीं है, और यह कहना कि वैष्णव दर्शन या शैवदर्शन के अनुसार चिन्तन से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, कट्टरता है और ईश्वर की अवमानना है. अमित, अनंत, विभु, सत्य स्वरूप अन्तर्यामी ईश्वर के समस्त भाव स्वात्मभाव से परिपूर्ण होते हैं, इसलिए ईश्वर के स्वरूप के चिन्तन में आप पूर्णत: स्वतंत्र हैं. यहाँ भाषा की भी कोई सीमा नहीं हो सकती कि संस्कृत में स्तोत्र गाने से ही ईश्वर प्रसन्न होगा. दक्षिण भारत के तमिल भाषा में रचित तोलकाप्पियम्, एतुत्तौके, पत्तुप्पातु, पदिनेकिल्लकणक्कु इत्यादि ग्रंथ तथा शिलप्पादिकारम्, मणिमेखलै इत्यादि महाकाव्य मन्त्र जैसे ही हैं. जिस तरह उत्तर भारत के हिन्दू रामचरित मानस की चौपाई का परायण करता है, उसी तरह उपरोक्त दक्षिण भारत के तमिल हिन्दू तमिल ग्रन्थों का पाठ करता है. लेकिन निःसंदेह वो मन्त्र की कोटि में नहीं रखे जा सकते. मन्त्र की परिभाषा एकदम अलग है. मन्त्र मननात्मक होते हैं “मननात् त्रायते इति मंत्र:” अथवा मननत्राण संयुक्तो मन्त्र इत्यभिधीयते” जबकि स्तुतियों का उस तरह से मनन नहीं किया जा सकता है. मन्त्र का प्रयोजन है स्वात्म तत्वमय परमधाम तक पहुंचना इसलिए यह मन से प्रारम्भ होता है. मन्त्र जप में मानसिक जप को इसीलिए सर्वोत्तम कहा गया है. जब आप मन से नीचे उतरते हैं तो आप वाणी के स्तर पर आते हैं, और जब वाणी के द्वारा इसका वर्णन करते हैं तो ईश्वर के स्वरूप को विकृत करते हैं. यही बात पुष्पदंत लिखते हैं ” अतीतः पंथानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः/ रतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि ।” और यही बात भगवद्गीता में भी कही गई है “आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन-माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः।” कोई इस अन्तर्यामी को आश्चर्यवत देखता है और वैसे ही अन्य कोई इसका आश्चर्यवत वर्णन करता है तथा अन्य कोई इसको आश्चर्यवत सुनता है; और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता. मन्त्र का “म” पाणिनि का अंतिम वर्ण है, प्रत्याहार यहीं से प्रारम्भ होता है. यह मनस है, मन है. यात्रा यहीं से प्रारम्भ होती है जब मनन से बुद्धियोग प्राप्त होता है तब वह त्राण कर देता है, मुक्त कर देता है. यही मन्त्र का अर्थ है.
“ॐ नम: शिवाय” या अघोर मन्त्र “ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः. सर्वेभ्यस् सर्व सर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्र रुपेभ्यो नम:” एक मन्त्र है जिसका मनन किसी स्तुति की तुलना में बेहतर ढंग से किया जा सकता है. महिम्न स्तोत्र में ‘अघोरान्नापरो मन्त्रो” कह कर इसे परम मन्त्र कहा गया है. चिन्मरिचियों का बीज, पिंड, मन्त्र, माला मन्त्र, स्तोत्र, कथा कुछ इसी क्रम से प्रसार है. वेदों का बीज है “प्रणव” अर्थात ॐ, इस प्रणव से ही गायत्री का प्राकट्य हुआ,गायत्री से वेदों का प्राकट्य हुआ, वेदों से संहिता, स्मृति, पुराण, इतिहास इत्यादि प्रकट हुए. इस प्रकार से देखें तो जो भी वांग्मय है वह मूलभूत रूप से मंत्रात्मक ही है. महर्षि पाणिनि को भगवान शिव से अ, इ ,उ ,ण्। ॠ ,ॡ ,क्,। ए, ओ ,ङ्। ऐ ,औ, च्। ह, य ,व ,र ,ट्। इत्यादि कुल 14 सूत्र प्राप्त हुए और इन्हीं से सम्पूर्ण व्याकरण है. सूत्र भी मंत्रात्मक ही होते हैं क्योंकि एक किसी सूत्र में ईश्वर के स्वरूप का कथन किसी स्तुति की तुलना में ज्यादा बेहतर ठंग से किया जा सकता है. ईश्वर के बारे में उपनिषद कहती है “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स:” ईश्वर वाणी का विषय नहीं हो सकता, वाणी के प्रत्याहार से उसकी उपलब्धि होती है. “ॐ” बीज है और इसे ईश्वर का एकमात्र वाचक कहा गया है, यह पूर्ण है. इस बीज में चतुर्थ पाद में विश्रांति है. यह प्रत्याहार के बाद की प्रशांति है. ईश्वर के स्वरूप का जितने कम शब्दों में वर्णन किया जाय वही श्रेष्ठ है. आचार्यों ने इसीलिए सूत्रों की रचना की थी.
पुराण में भगवान की कथा है, परन्तु यदि पूछें कि किस भगवान की कथा है ? तो उत्तर यही होगा कि किसी सम्प्रदाय विशेष में जो भगवान की कल्पना है उसकी कथा है. यही सत्य है. लेकिन यहाँ क्या “कथा” वास्तव में ब्रह्मचरिया है? नहीं है. यह एक प्रकार से परवर्जन बन गया है जहाँ ईश्वर झरझराकर वीर्यपात करता है और ऋषि पत्नियाँ उससे गर्भ धारण कर लेती हैं अथवा पत्नी के अपहरण होने के बाद वह विलाप करते हुए वन वन पूछता फिरता है “हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी? ”
दूसरी तरफ जब कोई कवि कविता के शिखर पर पहुंचता है तब उसकी कविता भी मंत्रात्मक हो जाती है. उस कविता में साम का प्राकट्य हो जाता है. इसी बात को वाल्मीकि रामायण के प्रारम्भ में वाल्मीकि के छंद को ‘मंगल श्लोक’ कह कर उसकी प्रसंशा की गई है. जब वाणी विकसित होती है. तब उससे दिव्य कविताओं का जन्म होता है.
संस्कृत की सुंदर स्तुतियाँ सुंदर कविताएँ हैं. मां सरस्वती की ये दो स्तुतियाँ एक संस्कृत में है दूसरी हिंदी में है और दोनों अपने स्तर पर मंत्रात्मक बन गईं हैं लेकिन हम इन्हें मन्त्र नही कह सकते-
या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना |
या ब्रह्माच्युत शंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥
और हिंदी में महाकवि निराला की यह स्तुति –
वर दे, वीणावादिनि वर दे!
प्रिय स्वतंत्र-रव अमृत-मंत्र नव
भारत में भर दे!
काट अंध-उर के बंधन-स्तर
बहा जननि, ज्योतिर्मय निर्झर;
कलुष-भेद-तम हर प्रकाश भर
जगमग जग कर दे!
नव गति, नव लय, ताल-छंद नव
नवल कंठ, नव जलद-मन्द्ररव;
नव नभ के नव विहग-वृंद को
नव पर, नव स्वर दे!
वर दे, वीणावादिनि वर दे।
देवता अन्तर्यामी रूप से हृदय में अवस्थित है, हृदय ही उसका सदन है. मन्त्र का प्रयोजन इस सदन तक पहुंच कर देवता का दर्शन करना है. मन्त्र द्वारा देवता की वांग्मयी पूजा से मनोमयी पूजा में प्रविष्ट होकर चैतन्यस्वरूप ईश्वर की चिच्छक्ति में समाहित हो जाना ही प्रयोजन है. सभी मन्त्र इस चिच्छक्ति की ही आख्या है.