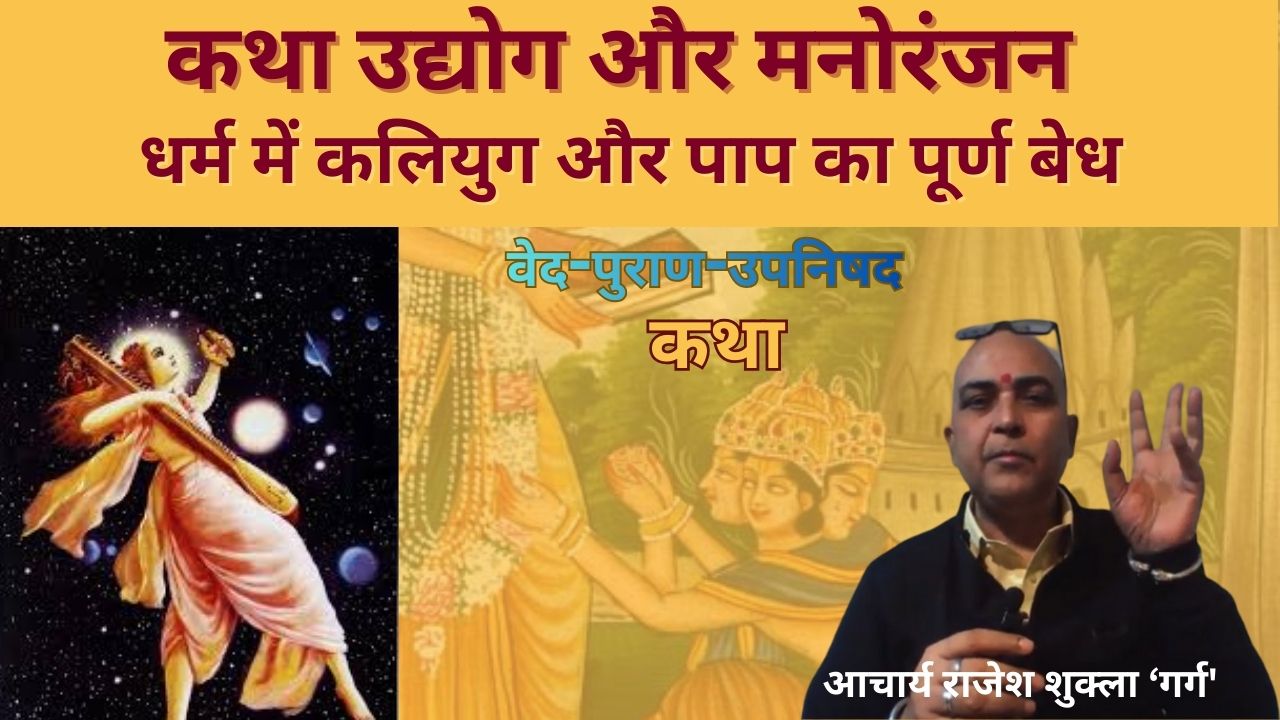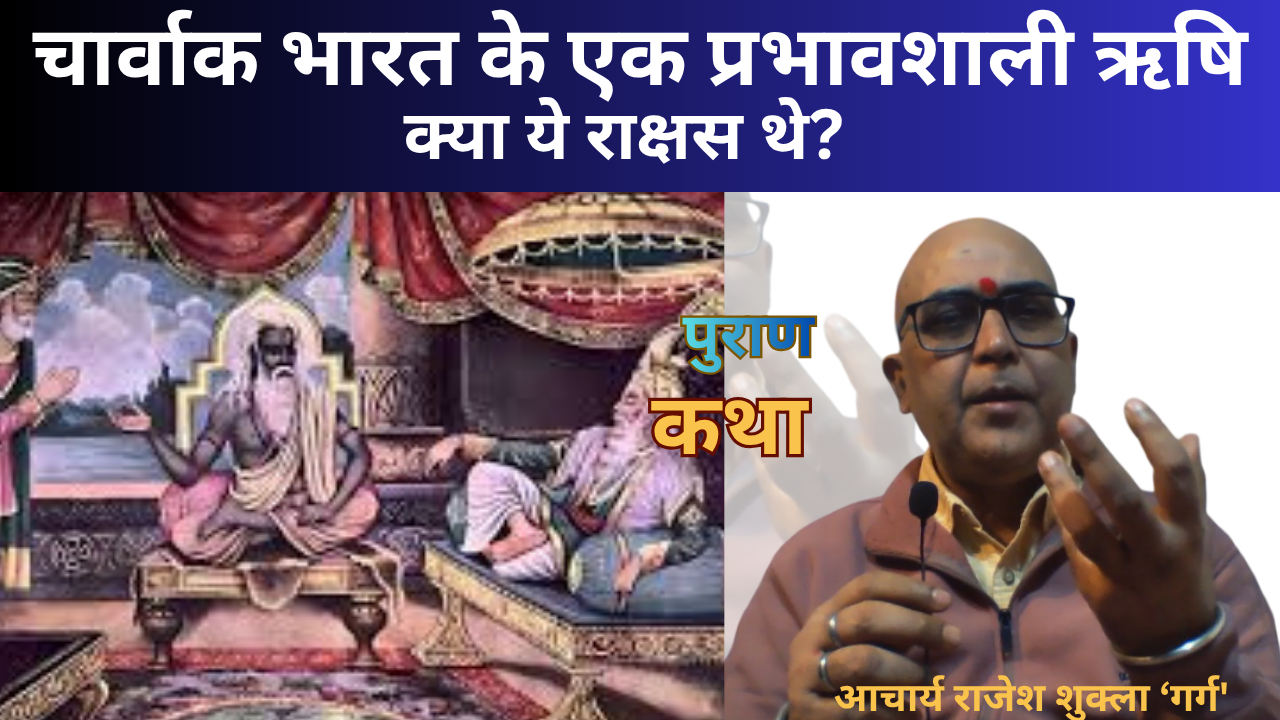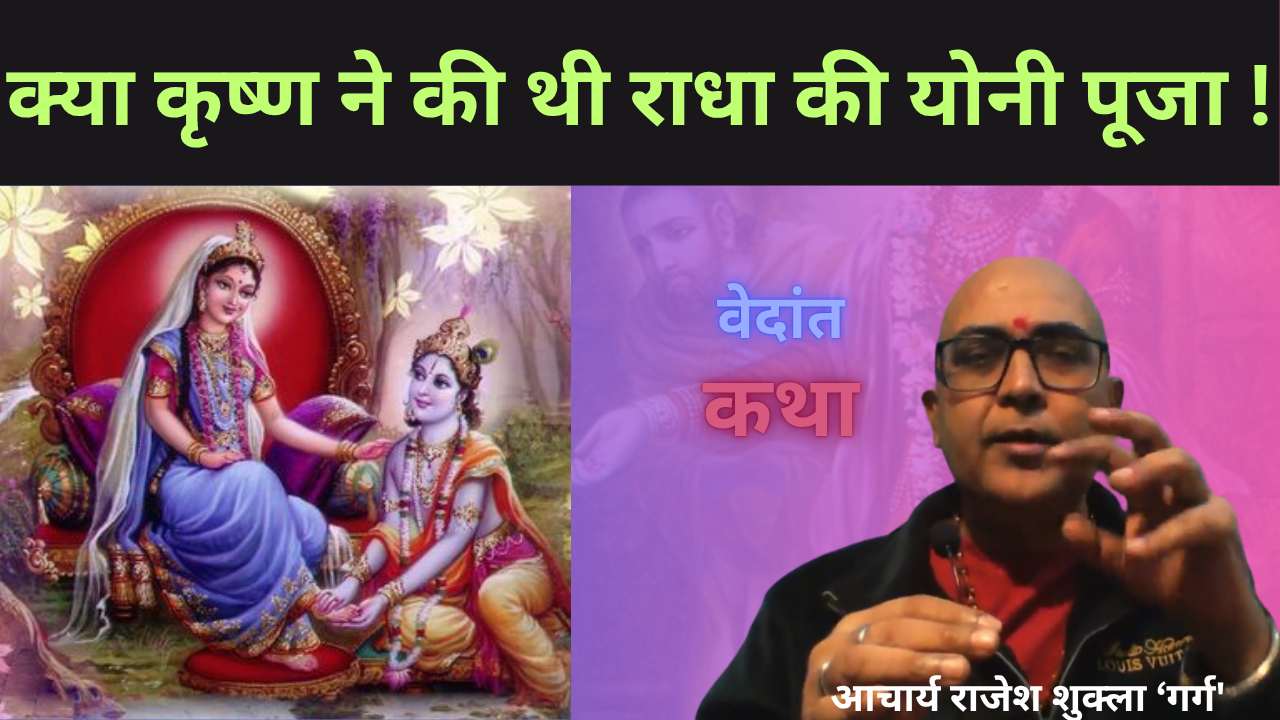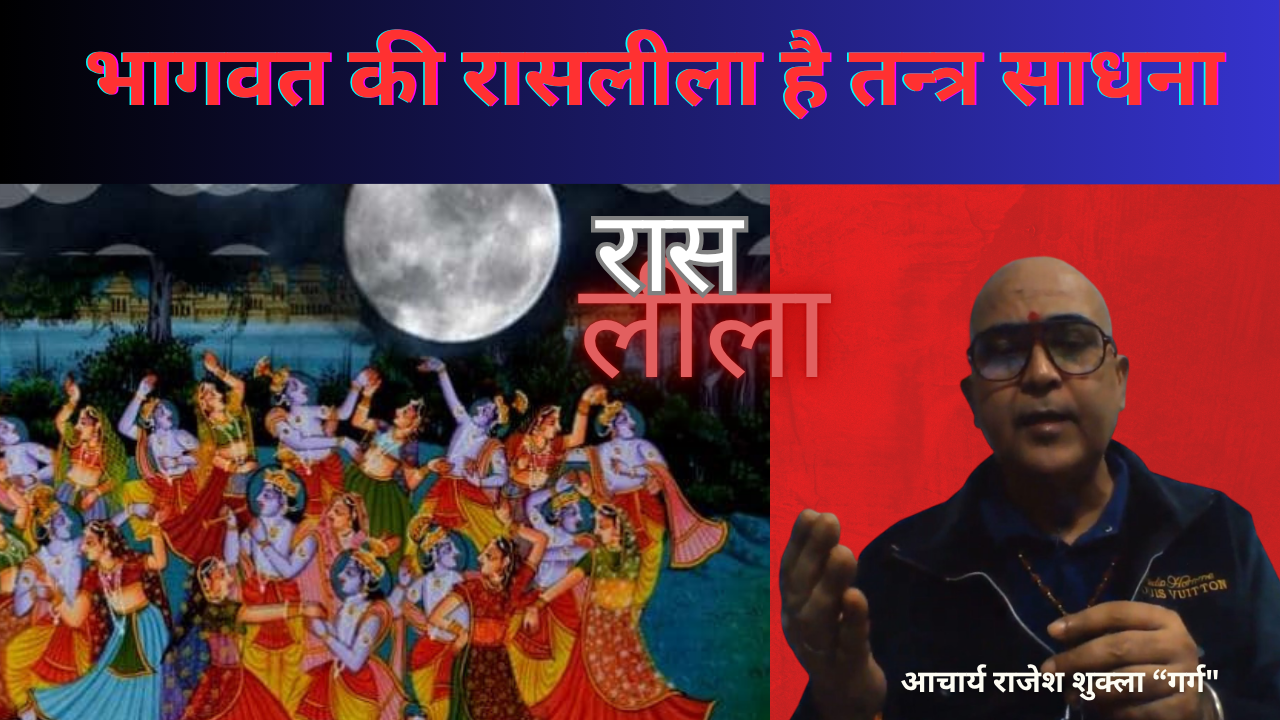महाभारत की कथा सर्पो और पक्षियों की कथा से ही शुरू होती है। सर्प और पक्षी सृष्टि की उत्पत्ति में पहले प्रमुख जीव है। आधुनिक सिद्धांत में भी विकास क्रम में सबसे उन्नत प्रारम्भिक जीव की प्रजाति सर्प और पक्षी ही हैं। मनुष्य का विकास सरीसृप से हुआ इसलिए रीढ़ रज्जू सर्पाकार है। खैर इस मुद्दे पर कभी और समय मिला तो लिखा जायेगा, फ़िलहाल महाभारत की सर्प की कथा पर आते हैं। सर्पो की रक्षा करने वाले जरत्कारू का कोई न कोई सम्बन्ध पूर्व काल में सर्प जाति से रहा होगा इसलिए यह कथा महत्वपूर्ण है। सर्पों से पांडवों का भी गहरा सम्बन्ध रहा, अर्जुन ने नाग जाति की कन्या से शादी किया था। नाग लोक के वासी पांडवों के मित्र रहे लेकिन कालान्तर में शाप वश ये दुश्मन हो गये। जन्मेजय के सार्प सत्र में महाभारत काल के सभी बड़े ब्राह्मण उपस्थित थे। नागों के राजा वासुकी को अपनी माता कद्रू के श्राप से भय था कि इस यज्ञ में साँपों का समस्त कुल नष्ट हो जाएगा। पूर्वकालमें नागमाता कद्रूने सर्पोंको यह शाप दिया था कि सर्पों को जनमेजयके यज्ञमें अग्नि भस्म कर डालेगी। वासुकी इससे बचने का उपाय पूछने अन्य प्रमुख साँपों के साथ ब्रह्मा की शरण में गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि नागों को जरत्कारू का पुत्र ही बचा सकता है। जरत्कारु यदि पुत्र की कामना करे तो ही नाग कुल बच सकता है। ब्रह्मा जी ने जरत्कारू की प्रतीक्षा करने के लिए कहा। परीक्षित को ब्राह्मण शाप का दोष था लेकिन जिस कुल में जरत्कारू का जन्म हुआ वह कुल भी कहीं न कहीं सांप के श्राप से पीड़ित था। जरत्कारु की कथा यहीं से शुरू होती है। जरत्कारू यायावर ऋषियों के गोत्र में जन्मा एक तपस्वी ब्राह्मण था. जरत्कारू किसका पुत्र था यह महाभारत में नहीं बताया गया है और कथा के लिए जरूरी भी नहीं है। कथा तो शून्य से भी प्रकट हो सकती है।
शौनक ऋषि जिनका जन्म अपने ही कुल से हुआ था और जिनकी जन्म कथा में सांप की कथा भी आती है, उन्हें ही यह कथा सुनाई गई है. शौनक के पिता रुरु मुनि सांपो को मारते रहते थे क्योंकि सांप ने उनकी पत्नी को डंस लिया था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण रुरु किसी विशाल वनमें गया, वहाँ उसने डुण्डुभ जातिके एक बूढ़े साँपको सोते देखा। उसे देखते ही उसके क्रोधका पारा चढ़ गया और उस ब्राह्मणने उस समय सर्पको मार डालनेकी इच्छासे कालदण्डके समान भयंकर डंडा उठाया। तब डुण्डुभ सर्प मनुष्य की भाषा में कहने लगा- ‘रुक जाओ रुरु, हमे क्यों मारते हो. रुरु बोला—सर्प! मेरी प्राणोंके समान प्यारी पत्नीको एक साँपने डँस लिया था। उसी समय मैंने यह घोर प्रतिज्ञा कर ली कि जिस-जिस सर्पको देख लूँगा, उसे-उसे अवश्य मार डालूँगा। उसी प्रतिज्ञाके अनुसार मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ। अतः आज तुम्हें अपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़ेगा। डुण्डुभ ने कहा- अहो! आश्चर्य है, बेचारे डुण्डुभ अनर्थ भोगनेमें सब सर्पोंके साथ एक हैं; परंतु उनका स्वभाव दूसरे सर्पोंसे भिन्न है तथा दुःख भोगनेमें तो वे सब सर्पोंके साथ एक हैं; किंतु सुख सबका अलग-अलग है। तुम धर्मज्ञ हो, अतः तुम्हें डुण्डुभों की हिंसा नहीं करनी चाहिये। रुरु ने जब उसकी बात सुनी तो उसने समझा कि यह कोई श्राप के कारण सर्प बना महात्मा है। उसने पूछा -भुजंगम! बताओ, इस विकृत (सर्प)-योनि में पड़े हुए तुम कौन हो? सर्प ने कहा- रुरो! मैं पूर्वजन्ममें सहस्रपाद नामक ऋषि था; किंतु एक ब्राह्मणके शाप से मुझे सर्प योनि में आना पड़ा है। रुरुने पूछा—भुजगोत्तम! उस ब्राह्मणने किसलिये कुपित होकर तुम्हें शाप दिया? तुम्हारा यह शरीर अभी कितने समय तक रहेगा? सर्प ने कहा- वह मेरा मित्र था, वह महान् तपोबलसे सम्पन्न होकर भी बहुत कठोर वचन बोला करता था। एक दिन वह अग्निहोत्रमें लगा हुआ था। मैंने खिलवाड़ में तिनकोंका एक सर्प बनाकर उसे डरा दिया। वह भयके मारे मूर्च्छित हो गया। होश आने पर क्रोधित उसने श्राप देते हुए कहा-अरे! तूने मुझे डरानेके लिये जैसा अल्प शक्तिवाला सर्प बनाया था, मेरे शापवश ऐसा ही अल्प शक्तिसम्पन्न सर्प तुझे भी होना पड़ेगा’। मैं उसकी तपस्याका बल जानता था, अतः मेरा हृदय अत्यन्त उद्विग्न हो उठा और बड़े वेगसे उसके चरणोंमें प्रणाम करके, हाथ जोड़, सामने खड़ा हो गया और उस तपस्वी से बोला—सखे! मैंने परिहासके लिये सहसा यह कार्य कर डाला था। ब्रह्मन्! इसके लिये क्षमा करो और अपना यह शाप लौटा लो। मुझे अत्यन्त घबराया हुआ देखकर सम्भ्रममें पड़े हुए उस तपस्वीने बार-बार गरम साँस खींचते हुए कहा—‘मेरी कही हुई यह बात किसी प्रकार झूठी नहीं हो सकती’। लेकिन तुम मुक्त जो सकते हो। इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो-‘भविष्यमें महर्षि प्रमतिके पवित्र पुत्र रुरु उत्पन्न होंगे, उनका दर्शन करके तुम्हें शीघ्र ही इस शापसे छुटकारा मिल जायगा’।
ऐसा जान पड़ता है तुम वही रुरु नामसे विख्यात महर्षि प्रमतिके पुत्र हो। अब मैं अपना स्वरूप धारण करके तुम्हारे हितकी बात बताऊँगा। इतना कहकर सहस्रपाद ने डुण्डुभ सर्प का रूप त्यागकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। सहस्रपाद ने रुरु को अहिंसा का उपदेश किया और बताया कि कैसे पहले राजा जनमेजयके यज्ञमें सर्पोंकी बड़ी भारी हिंसा हुई और उसी सर्पसत्रमें तपस्याके बल-वीर्यसे सम्पन्न, वेद वेदांगोंके पारंगत विद्वान् विप्रवर आस्तीक नामक ब्राह्मणके द्वारा भयभीत सर्पोंकी प्राणरक्षा हुई। सर्पों की इस कथा को घर पहुंच कर रुरु ने अपने पिता से सुना। उसी कथा को आगे सुत जी से शौनक सुन रहे हैं –
सुत जी ने कहा- शौनकजी! यह आस्तीक मुनिका उपाख्यान सब पापोंका नाश करनेवाला है। आपके पूछनेपर मैं इसका पूरा-पूरा वर्णन कर रहा हूँ। आस्तीकके पिता प्रजापतिके समान प्रभावशाली थे। ब्रह्मचारी होनेके साथ ही उन्होंने आहारपर भी संयम कर लिया था। वे सदा उग्र तपस्यामें संलग्न रहते थे। उनका नाम था जरत्कारु। वे ऊर्ध्वरेता और महान् ऋषि थे। यायावरों में उनका स्थान सबसे ऊँचा था। वे धर्मके ज्ञाता थे। एक समय तपोबलसे सम्पन्न उन महाभाग जरत्कारुने यात्रा प्रारम्भ की। वे मुनि-वृत्तिसे रहते हुए जहाँ शाम होती वहीं डेरा डाल देते थे। वे सब तीर्थोंमें स्नान करते हुए घूमते थे। उन महातेजस्वी मुनिने कठोर व्रतोंकी ऐसी दीक्षा लेकर यात्रा प्रारम्भ की थी, जो अजितेन्द्रिय पुरुषोंके लिये अत्यन्त दुःसाध्य थी। वे कभी वायु पीकर रहते और कभी भोजनका सर्वथा त्याग करके अपने शरीरको सुखाते रहते थे। उन महर्षि ने निद्रापर भी विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिये उनकी पलक नहीं लगती थी। इधर-उधर विचरण करते हुए वे प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी जान पड़ते थे। घूमते-घूमते किसी समय उन्होंने अपने पितामहोंको देखा जो ऊपरको पैर और नीचेको सिर किये एक विशाल गड्ढे में लटक रहे थे। उन्हें देखते ही जरत्कारुने उनसे पूछा—‘आपलोग कौन हैं, जो इस गड् ढेमें नीचेको मुख किये लटक रहे हैं ॥
वीरणस्तम्बके लग्नाः सर्वतः परिभक्षिते ।
मूषकेन निगूढेन गर्तेऽस्मिन् नित्यवासिना ॥
‘आप जिस वीरणस्तम्ब (खस नामक तिनकोंके समूह) -को पकड़कर लटक रहे हैं, उसे इस गड् ढेमें गुप्तरूपसे नित्य निवास करनेवाले चूहेने सब ओरसे प्रायः खा लिया है’ ।
पितर बोले—ब्रह्मन्! हमलोग कठोर व्रतका पालन करनेवाले यायावर नामक मुनि हैं। अपनी संतान-परम्पराका नाश होनेसे हम नीचे—नरक में गिरने वाले हैं। हमारी एक संतति बच गयी है, जिसका नाम है जरत्कारु। हम भाग्यहीनोंकी वह अभागी संतान केवल तपस्यामें ही संलग्न है। अतः वंश परम्परा का विनाश होनेसे हम यहाँ इस गड्ढेमें लटक रहे हैं। हमारी रक्षा करने वाला वह वंशधर मौजूद है, तो भी पापकर्मी मनुष्योंकी भाँति हम अनाथ हो गये हैं। साधुशिरोमणे! तुम कौन हो जो हमारे बन्धु-बान्धवोंकी भाँति हम लोगों की इस दयनीय दशाके लिये शोक कर रहे हो? ब्रह्मन्! हम यह जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो जो आत्मीय की भाँति यहाँ हमारे पास खड़े हो? सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ! हम शोचनीय प्राणियोंके लिये तुम क्यों शोकमग्न होते हो?
जरत्कारुने कहा—महात्माओ! आप लोग मेरे ही पितामह और पूर्वज पितृगण हैं। स्वयं मैं ही जरत्कारु हूँ। बताइये, आज आपकी क्या सेवा करूँ ?
पितर बोले—तात! तुम हमारे कुलकी संतान-परम्पराको बनाये रखनेके लिये निरन्तर यत्नशील रहकर विवाहके लिये प्रयत्न करो। प्रभो! तुम अपने लिये, हमारे लिये अथवा धर्मका पालन हो, इस उद्देश्यसे पुत्रकी उत्पत्तिके लिये यत्न करो।
न हि धर्मफलैस्तात न तपोभिः सुसंचितैः ।
तां गतिं प्राप्नुवन्तीह पुत्रिणो यां व्रजन्ति वै ॥
तात! पुत्रवाले मनुष्य इस लोकमें जिस उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं, उसे अन्य लोग धर्मानुकूल फल देनेवाले भलीभाँति संचित किये हुए तपसे भी नहीं पाते ॥ अतः बेटा! तुम हमारी आज्ञासे विवाह करनेका प्रयत्न करो और संतानोत्पादनकी ओर ध्यान दो। यही हमारे लिये सर्वोत्तम हितकी बात होगी।
जरत्कारुने कहा—पितामहगण! मैंने अपने मनमें यह निश्चय कर लिया था कि मैं जीवनके सुख-भोगके लिये कभी न तो पत्नीका परिग्रह करूँगा और न धनका संग्रह ही; परंतु यदि ऐसा करनेसे आपलोगोंका हित होता है तो उसके लिये अवश्य विवाह कर लूँगा। किंतु एक शर्तके साथ मुझे विधिपूर्वक विवाह करना है। यदि उस शर्तके अनुसार किसी कुमारी कन्याको पाऊँगा, तभी उससे विवाह करूँगा, अन्यथा विवाह करूँगा ही नहीं । (वह शर्त यों है—) जिस कन्याका नाम मेरे नामके ही समान हो, जिसे उसके भाई-बन्धु स्वयं मुझे देनेकी इच्छासे रखते हों और जो भिक्षाकी भाँति स्वयं प्राप्त हुई हो, उसी कन्या का मैं शास्त्रीय विधिके अनुसार पाणिग्रहण करूँगा। विशेष बात तो यह है कि मैं दरिद्र हूँ, भला मुझे माँगने पर भी कौन अपनी कन्या पत्नीरूप में प्रदान करेगा? इसलिये मेरा विचार है कि यदि कोई भिक्षा के तौरपर अपनी कन्या देगा तो उसे ग्रहण करूँगा। इस प्रकार मिली हुई पत्नीके गर्भसे यदि कोई प्राणी जन्म लेगा तो वह आपलोगोंका उद्धार करेगा, अतः आप मेरे पितर अपने सनातन स्थानपर जाकर वहाँ प्रसन्नतापूर्वक रहें।
उग्रश्रवाजी कहते हैं—तदनन्तर वे कठोर व्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण भार्याकी प्राप्तिके लिये इच्छुक होकर पृथ्वीपर सब ओर विचरने लगे; किं तु उन्हें पत्नीकी उपलब्धि नहीं हुई।
स कदाचिद् वनं गत्वा विप्रः पितृवचः स्मरन् ।
चुक्रोश कन्याभिक्षार्थी तिस्रो वाचः शनैरिव ॥
एक दिन किसी वनमें जाकर विप्रवर जरत्कारुने पितरोंके वचनका स्मरण करके कन्याकी भिक्षाके लिये तीन बार पुकार लगायी—‘ अरे, कोई है। क्या कोई भिक्षारूपमें मुझे कन्या दे सकता है’।
ब्रह्मा जी के कहे अनुसार सर्प इसी दिन का इन्तेजार कर रहे थे कि कब जरत्कारू के मन में पुत्र पैदा करने की ईच्छा जगेगी। जरत्कारू की पुकार सुनकर नागो के राजा वासुकी अपनी बहिनको लेकर मुनिकी सेवामें उपस्थित हो गये और बोले, ‘यह भिक्षा ग्रहण कीजिये।’ किंतु उन्होंने यह सोचकर कि शायद यह मेरे-जैसे नामवाली न हो, उसे तत्काल ग्रहण नहीं किया । उन्होंने संकल्प लिया था उनके नाम वाली कन्या का ही वे पत्नी के रूप में वरण करेंगे. जरत्कारुने पूछा—‘नागराज! सच-सच बताओ, तुम्हारी इस बहिनका क्या नाम है? वासुकि ने कहा—जरत्कारो! यह मेरी छोटी बहिन जरत्कारु नामसे ही प्रसिद्ध है। इस सुन्दर कटिप्रदेशवाली कुमारीको पत्नी बनानेके लिये मैंने स्वयं आपकी सेवामें समर्पित किया है। इसे स्वीकार कीजिये। द्विजश्रेष्ठ! यह बहुत पहलेसे आपहीके लिये सुरक्षित रखी गयी है, अतः इसे ग्रहण करें। जरत्कारू ने जरत्कारू को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया लेकिन दो शर्ते रखी। पहला कि जरत्कारू कभी उनसे कोई प्रश्न नहीं करेगी, जिस दिन प्रश्न करेगी उस दिन उसका त्याग कर देंगे। दूसरा-मै कोई कर्म नहीं करूंगा, मेरा भरण पोषण करना होगा। वासुकी सर्पों का राजा था उसने दोनों बातें स्वीकार कर ली। जरत्कारू वासुकी के महल में ही रहने लगे। समय के साथ जरत्कारू के गर्भ से आस्तिक का जन्म हुआ। जरत्कारू सूर्य का उपासक था। सर्पों का सूर्य से गहरा सम्बन्ध है। वैदिक काल से ही यह सम्बन्ध स्थापित है और भागवत पुराण में सूर्य के साथ चलने वाले सर्पों का वर्णन विस्तार से किया गया है। एकदिन जरत्कारु सायं के समय सो रहे थे। यह देख नागकन्या ने सोचा ऋषि सोये रहे तो उनकी संध्या वन्दन का लोप हो जायेगा, जरत्कारू ने उन्हें जगाया -उठिए आर्य ! सायं हो रही है, क्या सूर्योपस्थान नहीं करेंगे ? जरत्कारू ने उठते ही श्राप दिया – अरे, मूर्ख क्या तुझे नहीं पता मेरे सूर्योपस्थान के बगैर सूर्य अस्त नहीं होते ! इस प्रकार जरत्कारू ने पत्नी का त्याग कर दिया। उनके पुत्र आस्तीक वेद-वेदांगोंके पारंगत विद्वान्, तपस्वी, सब लोगोंके प्रति समानभाव रखनेवाले ऋषि बने तथा पितृकुल और मातृकुलके भयको दूर करनेवाले हुए। आस्तीक ने नागोंको संकटमुक्त किया। इसी प्रकार तपस्या तथा संतानोत्पादनद्वारा उन्होंने पितरोंका भी उद्धार किया।
कथा का सार ये है कि कालान्तर में ऋषि-मुनियों के लिए पुत्रोत्पत्ति सबसे प्रमुख मुद्दा रहा। उन्होंने इसके लिए कुछ भी किया चाहे सांप से ही शादी क्यों न करना पड़ा हो।