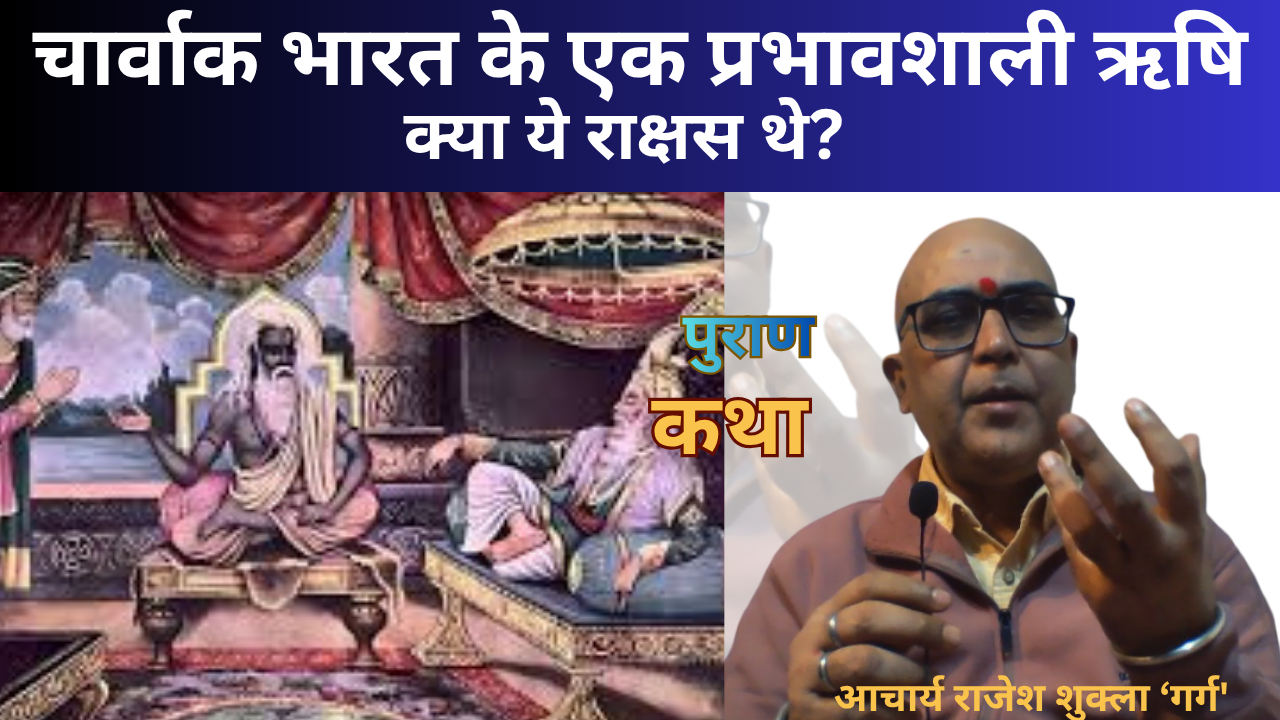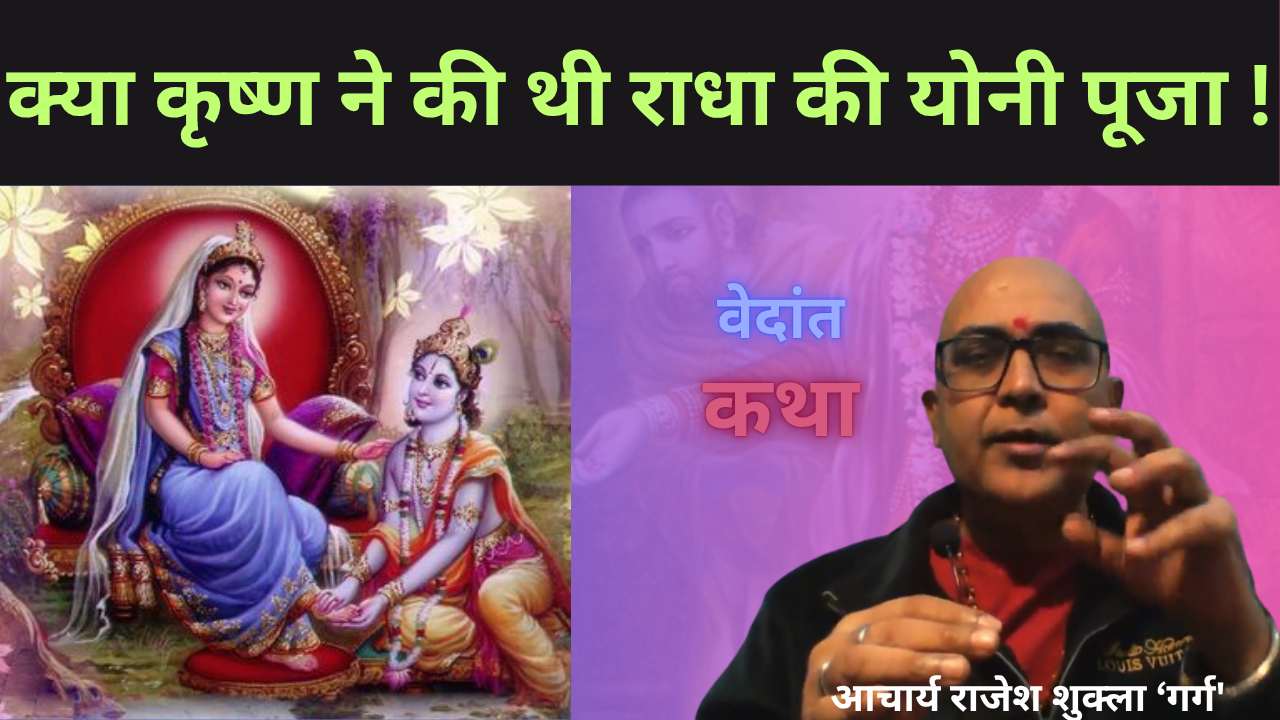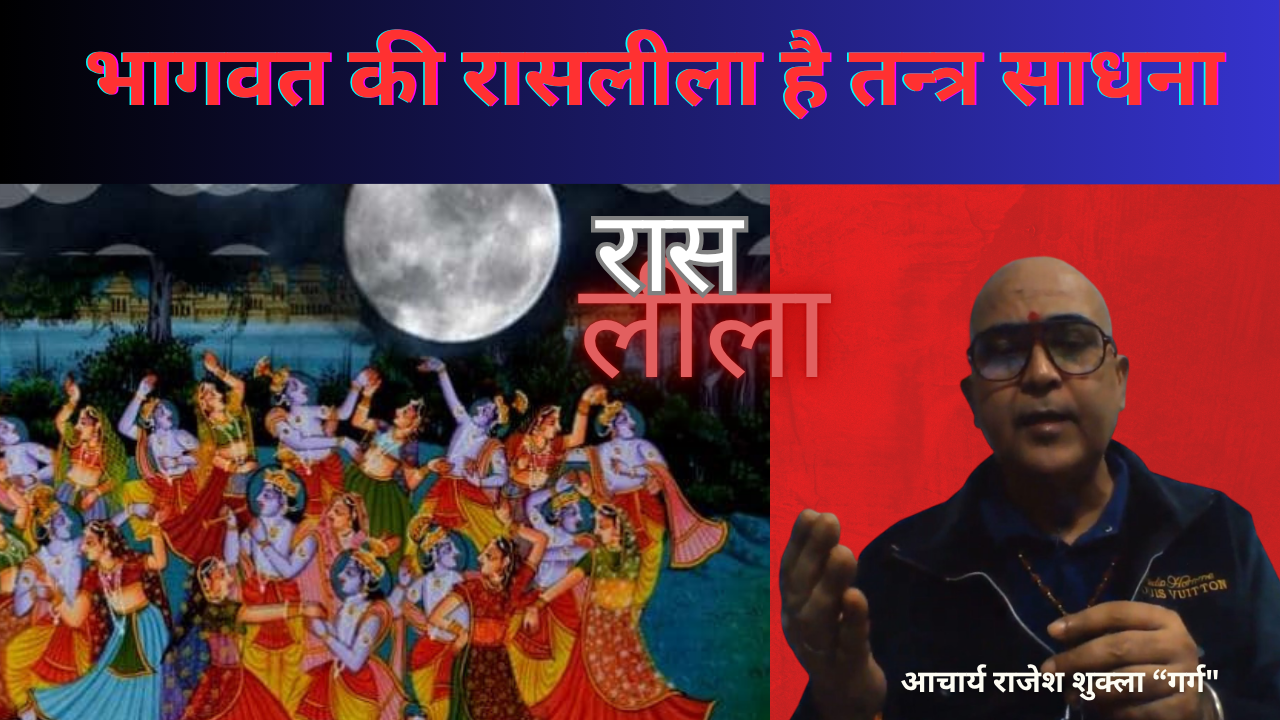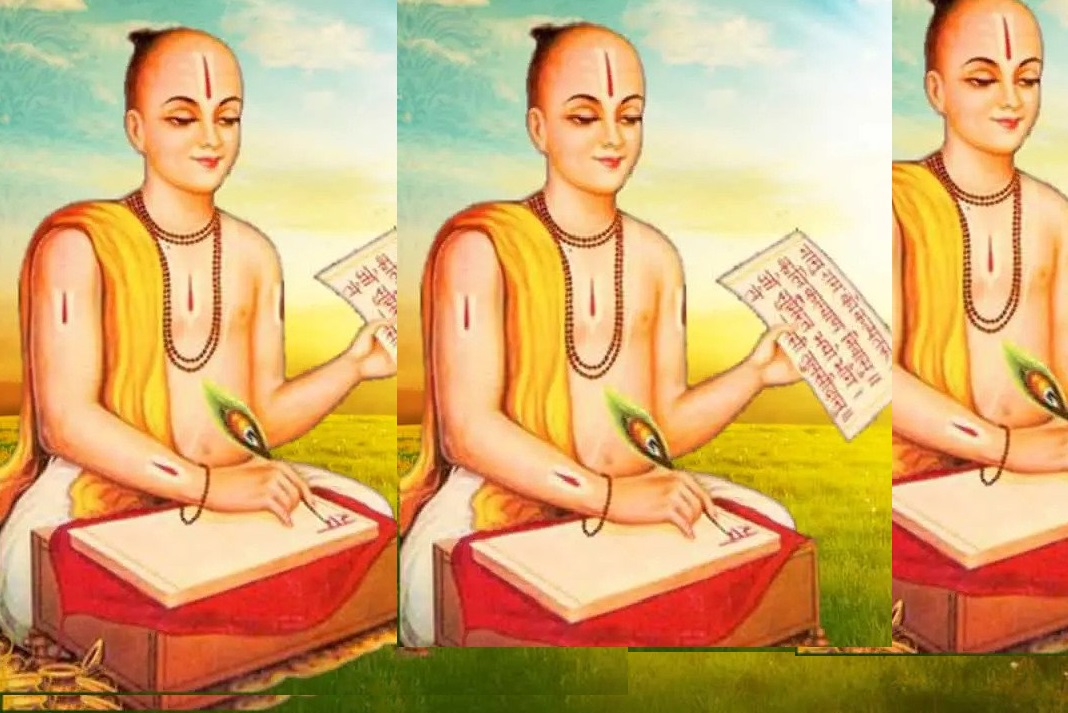
रामायणी वैष्णव सम्प्रदाय यह प्रारम्भ से ही प्रचारित कर रहा है कि ‘राम’ का नाम हिन्दुओं के दु:खों का अंत कर मुक्ति प्रदान कर सकता है. शिव भी काशी में मृतकों के कान में ‘राम’ का नाम ही फूंकते हैं. शैव इस पर निःसंदेह आपत्ति जताएंगे और कहेंगे कि काशी में महादेव सिर्फ अपना मुक्ति मन्त्र फूंकते हैं बल्कि इसकी काशी में जरूरत भी नहीं पडती क्योंकि पुराणों में काशी में मरने मात्र से मुक्ति कही गई है. चलिए हम थोडा यह देखते हैं कि क्या रामचरितमानस काव्य द्वारा इस मन्त्र का प्रचार करने वाले कवि तुलसी दास के दुःख का अंत करने में यह मन्त्र सक्षम हुआ था ?
तुलसीदास को पत्नी द्वारा बुरा भला कहने और आर्थिक विपन्नता में वैराग्य हुआ था. विनयपत्रिका के नीचे दिए गये पदों में उन्होंने सच्चाई के साथ लिखा. तुलसीदास एक कवि हैं इसलिए उनमें धर्म को व्यापार बनाने वाले बाबाओं की तरह हिपोक्रेसी नहीं है –
दुखित देखि संतन कह्यो, सोचै जनि मन मोहूं
तो से पसु पातकी परिहरे न सरन गए रघुबर ओर निबाहूं ।।
तुलसी तिहारो भये भयो सुखी प्रीति-प्रतीति विनाहू ।
नाम की महिमा, सीलनाथ को, मेरो भलो बिलोकि, अबतें ।।
विनयपत्रिका अर्थात विनय (विनती) के पत्र. जैसे छोटा कर्मचारी किसी काम के लिए, छुट्टी के लिए, सेलरी में से लोन के लिए लिखता है. तुलसीदास सभी देवताओं से अपने कष्टों से निवृत्ति और भगवान की भक्ति की प्राप्ति दोनों के लिए विनती करते हैं, जैसे शिव से विनती करते हुए कहते हैं कि आप सर्व सौभाग्य के मूल हैं सानुकूल हो जाइए-
तज्ञमज्ञान पाथोधि घटसंभवं , सर्वगं सर्वसौभाग्यमूलं ।
प्रचुर भव भंजनं , प्रणत जन रंजनं , दास तुलसी शरण सानुकूलं ।।
लेकिन न ग्रह सानुकूल हुए और भगवान ने उनके कष्टों की निवृत्ति की. तुलसीदास का रुदन विनयपत्रिका से पहले की कविताओं में भी है और उसके बाद भी यह रुदन जारी रहता है. तुलसीदास बचपन से ही असहाय और दरिद्रता में रहे. दुःख ही उनके जीवन की सबसे बड़ी कथा है. उन्होंने लिखा है, “माता-पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया। विधाता ने भी मेरे भाल (भाग्य) में कोई भलाई नहीं लिखी-–मातु पिता जग जाइ तज्यो, विधि हू न लिखी कछु भाल भलाई। जैसे कुटिल कीट को पैदा करके छोड़ देते हैं, वैसे ही मेरे माँ-बाप ने मुझे त्याग दिया–तनु जन्यों कुटिल कीट ज्यों तज्यो माता पिता हूँ।
दुनिया में और कोई सहारा न पाकर उन्होंने राजा राम को चुना. असहाय मनुष्य के लिए और कौन सहारा हो सकता है? अयोध्या के राजा राम को उन्होंने अपना ईष्ट बना लिया. उनका पूरा विश्वास था कि राम ही दुःख दलनकर्ता गरीब निवाजू हैं, वही साहेब हैं. वे साहेब से याचना करते फिरे. कवितावली में लिखते हैं कि महाराज जिस पर कृपा कर दें उसकी दुःख दरिद्रता को क्षीण करके छोड़ते हैं अर्थात दुःख दरिद्रता का अंत कर देते हैं –
“केवल राम ही से मांगो
रीति महाराज की, नेवाजिए जो माँगनो सो.
दोष दुःख दारिद दरिद्र कै कै छोड़िये “
महाराज राम से पेट खोल खोल कर तुलसीदास मांगते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलता. उनकी कविताएँ एक दरिद्र की कविता है, बहुत व्यक्तिगत हैं; उनकी कविताओं में उनकी सांसारिक पीड़ाओं के निवारण की प्रार्थना और ईष्ट की कृपा की कामना ये दोनों ही बातें एकसाथ हैं. उनका मानना है कि राजा के यश के गुणगान करने से दोनों ही प्राप्त हो जाएगा क्योंकि राजा राम गरीब नवाज हैं. राजा का यशगान करने की यह मानसिकता सभी प्राचीन भारत के सभी कवियों में रही है.
तुलसीदास का जीवन बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा और उन्हें बनारस के पंडों और ब्राह्मणों ने बड़ा पीड़ित और अपमानित किया. समाज में भी गरीब का सम्मान कौन करता है? समाज ने भी दुत्कारा ही. तुलसीदास इस नीचे लिखे गये दोहे में जो कुछ भी कह रहे हैं, यह उनका भोगा हुआ यथार्थ है.
तुलसी सरनाम गुलामु है राम को, जाको, रुचै सो कहै कछु ओऊ।
माँगि कै खैबो, मसीत को सोईबो, लैबो को, एकु न दैबे को दोऊ॥
जिसको जो लगे सो कहे. मैं तो माँग के खा लूंगा और मस्जिद में सो लूंगा, न किसी से एक लेना है, न दो देना है. यहाँ मस्जिद का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि हिन्दू समाज ने उन्हें बड़ा अपमानित किया. गरीब तो कुत्ता ही होता है जिसे हर जगह से दुत्कार मिलती है इसलिए खुद को कुकुर कहना कोई बड़ी बात नहीं है. तुलसीदास की दरिद्रता और समाजिक दुत्कार ने उनको इतना तोड़ दिया कि उन्होंने खुद को कुत्ते से ज्यादा नहीं समझा. कुत्ते जैसा ही रहे , मालिक की दया पर पूर्ण निर्भर.
विनयपत्रिका, कवितावली इत्यादि में हर पद्य में विनय पूर्वक राजा राम का गुणगान करते हैं और मांगते ही रहे हैं. तुलसीदास बहुत भोले हैं, सोचते हैं ऐसे महाराज नहीं सुनते तो उनकी पत्नी से बात पहुंचा दो, तो विनयपत्रिका में राजा राम की पत्नी से विनय पूर्वक कहते हैं –
कबहुँक अंब, अवसर पाइ ।
मेरिऔ सुधि द्याइबी, कछु करुन – कथा चलाइ ॥१॥
दीन, सब अँगहीन, छीन, मलीन, अघी अघाइ ।
नाम लै भरै उदर एक प्रभु – दासी – दास कहाइ ॥२॥
बूझिहैं ‘ सो है कौन ‘, कहिबी नाम दसा जनाइ ।
सुनत राम कृपालुके मेरी बिगरिऔ बनि जाइ ॥३॥
कभी अवसर हो तो कुछ करुणाकी बात छेड़कर श्रीरामचन्द्रजीको मेरी भी याद दिला देना, ( इसीसे मेरा काम बन जायगा ) ॥ कहना कि एक अत्यन्त दीन, सर्व साधनोंसे हीन, मनमलीन, दुर्बल और पूरा पापी मनुष्य आपकी दासी ( तुलसी ) दास कहलाकर और आपका नाम ले – लेकर पेट भरता है ॥ इसपर प्रभु कृपा करके पूछें कि वह कौन है, तो मेरा नाम और मेरी दशा उन्हें बता देना । कृपालु रामचन्द्रजीके इतना सुन लेनेसे ही मेरी सारी बिगड़ी बात बन जायगी ॥
कवितावली में एक पद्य में स्वयं के निम्न वर्ग में पैदा होने पर भाग्य पर कोसते हैं (ब्राह्मण जाति में पैदा होने से वर्ग नहीं बदल जाता ? ब्राह्मण जाति में जो सम्पन्न वर्ग है वो निम्न वर्ग के गरीब ब्राह्मणों का शोषण ही करते हैं, उन्हें अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए भटकाते हो रहे हैं ) और लिखते हैं –
तुलसी बनि हैं राम ! रांवरे बनाये ना तो
धोबी कैसो कुकुर न घर को न घाट को ।।
ऊँचौ मनु, ऊँचौ रूचि, भागु नीच निपट हि
लोकरीति लायक न लंगर लबारु है ।।
स्वारथु अगमु परमारथ की कहाँ चली
पेट की कठिन जगु जीव को जवारु हैं ।।
हे राम! यदि आप बना दें तो ही मैं कुछ बन जाऊंगा अन्यथा धोबी के कुत्ते की तरह न घर का रहूँगा न घाट का रहूँगा.
रामचरितमानस के लिखे जाने से पूर्व तुलसीदास एक कवि के रूप में तो प्रतिष्ठित हो गये थे लेकिन रूलिंग क्लास के संस्कृत ब्राह्मणों में स्वीकार्यता नहीं थी इसलिए कवि के रूप में सम्मान तो था लेकिन उससे आर्थिक लाभ नहीं मिलता था. अपनी कवि के रूप में प्रतिष्ठा के बारे में लिखते हैं –
जाति के, सुजाति के, कुजाति के, पेटागि बस,
खाए टूँक सब के बिदित बात दुनी सो।
मानस बचन काय किए पाप सति‡ भाय,
राम को कहाय दास दगाबाज पुनी सो॥
राम नाम को प्रभाउ पाउ, महिमा प्रताप,
तुलसी से जग मानियत महामुनी सो।
अति ही अभागो अनुरागत न रामपद,
मूढ़ एतो बड़ो अचरज देखि- सुनी सो॥
पेट की अग्नि को शांत करने के लिए हमने जाति, कुजाति, अपनी जाति, सब से रोटी के टुकड़े मांग मांग कर खाए , सो बात दुनिया जानती है। मन, वचन, शरीर से पाप सहज ही (अनेक) किये, फिर राम का कहाकर भी दग़ाबाज़ रहा। रामनाम का प्रभाव और महिमा से तुलसी आज मनुष्य में बड़ा मुनि गिना जाता है।
जायो कुल मंगन, बधावनों बजायो सुनि,
भयो परिताप पाप जननी जनक को।
बारे तेँ ललात बिललात द्वार द्वार दीन,
जानत हौं चारि फल चारि ही चनक को॥
भीख मांगने वाले ब्राह्मणों के कुल में जनमा हूँ। जन्म का बधावा न बजा, जन्म सुनकर माता-पिता दोनों को पाप का परिताप हुआ। छोटे से, द्वार द्वार ललचाता रोता फिरता हूँ, दीन हूँ और चार चनों ही को चारों फल जानता हूँ अर्थात् चार चने मिल जाने से जानता हूँ कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल मिल गये।
तुलसी सो साहिब समर्थ को सुसेवक है,
सुनत सिहात सोच बिधि हू गलक को।
यदपि गरीबी से मुक्ति नहीं मिली लेकिन उनके हृदय में कविता का स्फुरण होने लगा था और इससे कवियों के बीच प्रतिष्ठा और सम्मान था. यह तुलसीदास के लिए कम संतोष की बात नहीं थी कि चलो धन भले न मिले कविता तो मिली. उनकी जितनी कविताएँ हैं वो रामायण लिखने की पूर्वपीठिका है. सब कवितायें छोटी बड़ी रामायण ही हैं. विनयपत्रिका तक आते आते उनकी ईच्छा अब बस ये ही रह गई थी कि धन मांगने का कोई फायदा नहीं, जीवन ऐसे ही चलता रहेगा.अब बस जो कविता चाहता हूँ वो मिल जाए ताकि मैं जो काव्य लिखना चाहता हूँ वो लिख सकूं यदपि की आर्थिक कष्ट और दुःख से मुक्ति की याचना भी एकदम से नहीं रुकी. तुलसीदास सभी देवी देवताओं से विनय करने लगते हैं कि राम की कृपा मिल जाए तो जो लिख रहा हूँ उसमे कोई बात आ जाएगी और मेरा काम बन जायेगा. राम-राम करने से तुलसीदास की दरिद्रता और पीडाओं का अंत नहीं हुआ लेकिन जिस तरह किसी कवि और लेखक को किसी रचना के लिखने से उसको मन में प्रसाद और संतोष होता है, उसी प्रकार तुलसीदास को इस बात से संतोष था कि कमसे कम मेरी कविता से मेरी संसार में पहचान तो है. विनयपत्रिका तक आते आते इनमें कविता प्रस्फुटित हो चुकी थी, उनमे एक लय है, साम का जन्म हो चूका था जो रामचरितमानस में प्रकट हुआ.
रामचरितमानस कवि की सिद्धि है लेकिन क्या इस सिद्धि के बाद भी राम ने तुलसीदास के सभी कष्टों का नाश किया? उन्हें अंतिम वर्षों में अतिशय शारीरिक कष्ट हुआ था। तुलसीदास बाहु की पीड़ा से व्यथित हो उठे तो असहाय बालक की भांति आराध्य को पुकारने लगे थे और हनुमान बाहुक लिखा –
घेरि लियो रोगनि कुजोगनि कुलोगनि ज्यौं,
बासर जलद घन घटा धुकि धाई है ।
बरसत बारि पोर जारिये जवासे जस,
रोष बिनु दोष, धूम-मूलमलिनाई है ।।
करुनानिधान हनुमान महा बलबान,
हेरि हैसि हांकि फूंकि फौजें तै उड़ाई है ।
खाए हुतो तुलसी कुरोग राढ़ राकसनि,
केसरी किसोर राखे बीर बरिआई है ।
(हनुमान बाहुक, ३५)
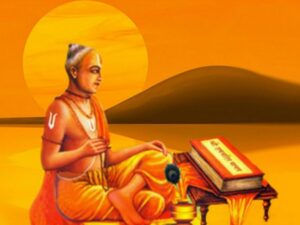
निम्नांकित पदों से तुलसीदास की तीव्र पीड़ानुभूति और उसके कारण शरीर की दुर्दशा का पता चलता हैं –
पायेंपीर पेटपीर बांहपीर मुंहपीर
जर्जर सकल सरी पीर मई है ।
देव भूत पितर करम खल काल ग्रह,
मोहि पर दवरि दमानक सी दई है ।।
हौं तो बिन मोल के बिकानो बलि बारे हीं तें,
ओट राम नाम की ललाट लिखि लई है ।
कुंभज के निकट बिकल बूड़े गोखुरनि,
हाय राम रा ऐरती हाल कहुं भई है ।।
पाँव की पीड़ा, पेट की पीड़ा , बांह की पीड़ा और मुख की पीड़ा- सारा शरीर पीड़ा से जर्जर हो रहा है. देवता, पितर, कर्म, काल, ग्रह सब एक साथ मुझ पर ताप दे रहे हैं मानों कष्टों की बाढ़ आ गई हो. मैंने राम नाम का आधार लिया है, हाय ! राजा राम जी क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि अगस्त्य मुनि का सेवक गाय के खुर में डूब गया हो !
दोहावली के तीन दोहों में बाहु-पीड़ा की अनुभूति –
तुलसी तनु सर सुखजलज, भुजरुज गज बर जोर ।
दलत दयानिधि देखिए, कपिकेसरी किसोर ।।
भुज तरु कोटर रोग अहि, बरबस कियो प्रबेस ।
बिहगराज बाहन तुरत, काढिअ मिटे कलेस ।।
बाहु विटप सुख विहंग थलु, लगी कुपीर कुआगि ।
राम कृपा जल सींचिए, बेगि दीन हित लागि ।।
तो तुलसीदास बाँहों में दर्द से कराहते हुए हनुमान से फूंक कर उड़ा देने के लिए कहते हैं जो हनुमान जी नहीं उड़ाते जैसे राम जी उनकी दुःख दरिद्रता नहीं खत्म करते. लेकिन रामायण कथा कर भांड की तरह रूपये कमाने वाले बाबा जनता से कहते रहते हैं कि कोई पीड़ा कष्ट हो तो बस 7 बार हनुमान बाहुक पढ़ लो पीड़ा का अंत हो जायेगा. तुलसीदास की पीडाओं से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था जब जिन्दा थे, जब मर गये तो भी उनके कष्टों की बात कोई नहीं करता ..इसे आस्था खत्म होती है. अरे, राम का इतना बड़ा भक्त दरिद्रता में मर गया ?
तुलसीदास को रामोपासना से कविता प्राप्त हुई और वे एक श्रेष्ठ काव्य की रचना कर पाए लेकिन इससे उन्हें धन नहीं मिला, उनकी दरिद्रता नहीं गई. क्यों ? क्योंकि वे आज के बाबाओं की तरह बाजार में वेश्या की तरह खुद को नहीं बेच रहे थे, वे साहित्यसाधना कर रहे थे. कविता से जब जनता एंटरटेनमेंट करती है तो कविता से धन प्राप्त होता है जैसे तुलसीदास के मरने के बाद तमाशाई बाबा नाच-गाना के साथ रामचरितमानस गा कर मनोरंजन करते हैं तो उन्हें एक कथा का लाखों प्राप्त होता है. आध्यात्म का बिजनेस से पैसे मिलते हैं, आध्यात्म से पैसे नहीं मिलते हैं. भगवद्गीता में ‘योगक्षेम’ वहन करने की बात परमात्मा ने किया है –
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।।9.22।।
अनन्य भाव से मेरा चिन्तन करते हुए जो भक्तजन मेरी ही उपासना करते हैं, उन नित्ययुक्त पुरुषों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ।।
तुलसीदास ने राम की उपासना अनन्यभावसे युक्त होकर किया और सभी कविताओं में भगवान से याचना करते फिरे लेकिन राम ने उन्हें कोई धन नहीं प्रदान किया. योगक्षेम का अर्थ है कि भिक्षा में मोटा कपड़ा अन्न मिलता रहेगा. तुलसीदास को मोटा अन्न कपड़ा मिलता रहा और बाद में उनको यह स्पष्ट हो गया कि हम रोज मांग कर गलत कर रहे थे. विनयपत्रिका तक आते आते उन्हें आध्यात्म का अर्थ समझ में आ गया और अब वे सिर्फ ईश्वर में भक्ति मांगने लगे क्योंकि यही मनुष्य को आत्यंतिक सुख दे सकता है और आनन्द की प्राप्ति करा सकता है. दोनों में से एक ही प्राप्त हो सकता है – संसार या निर्वाण . निर्वाण को सम्हार स्वरूप इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह हर कामनाओं का अत्यान्तिक निरोध है.
प्रेम गली अति सांकरी ता में दो न समाहि..
तुलसीदास जब तक मांगते रहे हैं “हे राम मेरी दरिद्रता खत्म करो, मेरे कष्टों को हर लो इत्यादि ” तब तक कविता का जन्म नहीं होता है, जब मांगना छोड़ देते हैं और ईश्वर से प्रेम की कामना करते हैं तब कविता प्रकट होती है. यह एक आध्यात्मिक बात है. परन्तु इसमें धर्म जैसा कुछ भी नहीं यदपि की तुलसीदास ने अपना ईश्वर राजा राम को मान कर अपने भीतर एक दरिद्र आध्यात्म का विकास किया. तुलसीदास के आध्यात्म को एक दरिद्र आध्यात्म कह सकते हैं. इस आध्यात्म ने उन्हें बड़ा विनयी बनाया ठीक वैसे ही जैसे एक लाचार-गरीब समाज में बड़ा विनयी हो जाता है “साहेब, बाबू भैया, मालिक, आप ही सब हो, हम तो आपके नौकर हैं, दास हैं. ” तुलसीदास का यह विनय दरिद्रता का आध्यात्म से उपजा. यह किताब ‘राम चरित मानस” हिन्दुओं में दास चेतना को पुष्ट करने का एक और बड़ा माध्यम बन गया. दरिद्रता के आध्यात्म की एकमात्र यही परिणिति है, वह आपको मन से भी राजा नहीं बनाता. इसी दरिद्रता के आध्यात्म के यात्री कवियों में महाकवि निराला भी थे.
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईश्वर की कौन छवि लेकर तुम चलते हो .. दांते एलीगियरी का सुप्रसिद्ध महाकाव्य डिवाइन कॉमेडिया है जिसमे कवि की आध्यात्मिक यात्रा में प्रमुख माध्यम उसकी प्रेमिका बिएट्रिस है. मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा में माध्यम कुछ भी हो सकता है लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि उसको किस स्तर तक जी पाते हो !
लेकिन जो मौलिक सवाल है कि क्या “राम” नाम व्यक्ति को मुक्त कर सकता है ? वैदिक धर्म की श्रुतियां कहेंगी नहीं कर सकता क्योंकि यह ईश्वर का वाचक नहीं है. भगवद्गीता में कृष्ण ये नहीं कहते कि अंतिम समय राम का नाम लेकर प्राण त्यागने से मुक्ति होती है –
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्। यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्।
ॐ इस एक अक्षर का स्मरण करते हुए जो देह का त्याग करता है उसे परम गति मिलती है. राम, कृष्ण, राधा, शंकर, राजेश, सुरेश, सुजाता, वृंदा सब नाम ईश्वर के ही है, सभी नाम ईश्वर के ही नाम हैं इसलिए चुने हुए कुछ 1000 नाम विष्णु के विष्णु सहस्र’नाम में हैं, तुम 10 हजार चुने हुए नाम भी बना सकते हो वो भी ईश्वर के नाम ही होंगे. लेकिन इन नामों की गति प्रणव जैसी नहीं है. जिस नाम की जहाँ तक गति वहां तक उसके जप करने वालों की गति है. प्रणव transcendental है.
राम का नाम तुलसीदास की दरिद्रता खत्म नहीं कर सकता इसलिए वह मुक्ति भी प्रदान करने में सक्षम नहीं है. यह वैष्णव सम्प्रदाय के रामायणी बहुत लम्बे समय से राम की छवि को गढ़ते रहे हैं और उससे मुक्ति होती है यह स्थापित करते रहे हैं. तुलसीदास का रामचरितमानस मरते हुए रामायणी सम्प्रदाय के लिए अमृत बन कर सामने आया और सम्प्रदाय इसपर सवार होकर चल पड़ा. बाबा रामायण कथा को उद्योग बनाकर करोड़ो कमा रहे हैं और उन्हें क्या चाहिए. लेकिन रामचरितमानस लिखना बड़ा कठिन है, कष्ट भोगना पड़ेगा जैसे तपस्या में कष्ट होता है.