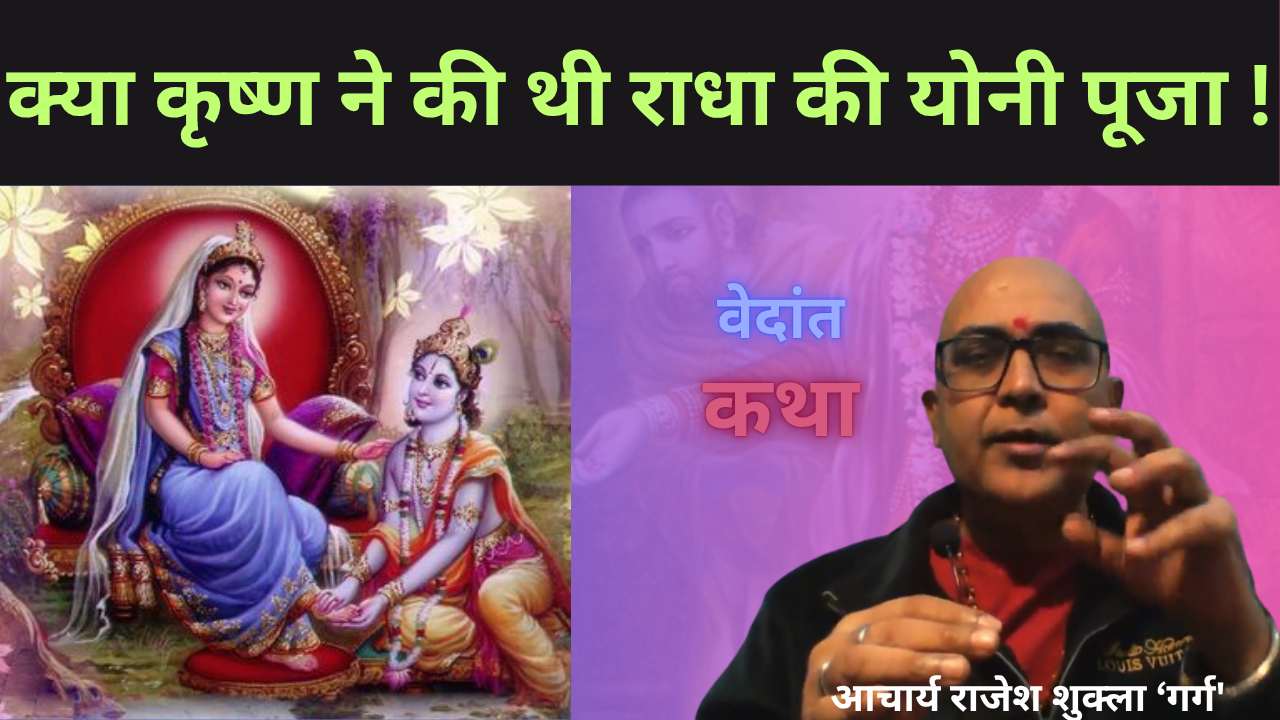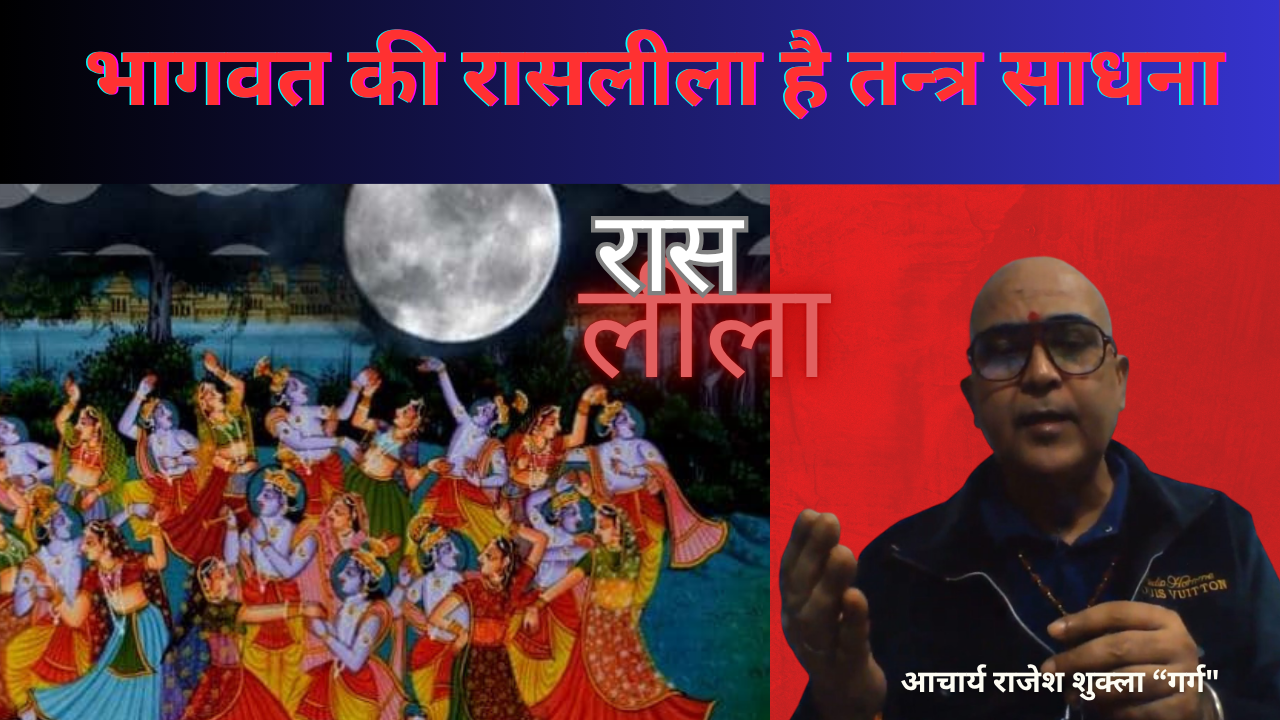हिन्दू धर्म में ज्यादातर व्रत की कथा में कोई राजा, साहूकार अथवा ब्राह्मण होते हैं। जीवन की किसी परेशानी के इदगिर्द ही ज्यादातर पुराणों में कथा गढ़ी गई हैं। पुराण से बाहर भी छोटी छोटी व्रत कथाएं छाप कर प्रचारित की गईं जिनमें राज्यवार अद्भुत विविधता है। यह कथाएं मूलभूत रूप से ज्योतिषीय सन्दर्भ रखती हैं तथा मास और तिथि के इदगिर्द बुनी गईं। भारत में जब ज्योतिष उन्नत हो गया और करण और महूर्त शास्त्र प्रचलन में आये उसके बाद तीर्थों में बैठे बाबाओं ने काम्य व्रत और उपवासों की झड़ी लगा दी। लगभग सभी पुराण व्रतों के महात्म्य से भर दिए गये। यह बहुत प्राचीन बात नहीं है। मसलन अनंत चतुर्दशी की कथा को यहाँ देखे और समझें। ब्राह्मण कौंडिन्य पर शनि की दशा कैसे आई और उसका निवारण कैसे हुआ। कथाओं को धर्म से जिस तरह मूर्खतापूर्ण तरीके से जोड़ा जाता है उसमे कोई तर्क नहीं होता। किसी विशेष देश काल में अर्थात किसी विशेष ज्योतिषीय योग में किया गया सात्विक धर्म, ईश्वर पूजन अथवा दान निःसंदेह आत्मकल्याण के लिए अच्छा होता है लेकिन अनंत व्रतों का कोई औचित्य तो नहीं है, इससे जनता में उन्माद और विकार ही पैदा होता है। राजा भोज द्वारा लिखित 11वीं शताब्दी के ग्रंथ राजमार्तण्ड केवल 24 व्रतों की पहचान करता है लेकिन उसके बाद बाबा लोग 33 करोड़ देवी-देवताओं के अनुसार व्रत बनाने में जुट गये और वर्तमान में हर महीने में एकादशी सहित लगभग 10-12 व्रत रहते हैं, जिनमे कभी कभी किसी दिन दो दो या तीन व्रत भी रहते हैं। 12वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ कृत्यकल्पतरु में लगभग 175 व्रत का वर्णन हैं। इसके उपरांत लगभग सब देवताओं की जयंती हैं, सब ग्रहों की जयंती और व्रत है। जो पर्व और त्यौहार हैं वो अलग हैं, व्रत उनमे भी होता ही है। पौराणिकों का मुहूर्तशास्त्र भी अद्भुत है जो किसी त्यौहार की तिथि का निर्णय नहीं कर पाता, उनके गैंग बने हुए हैं जो अपनी श्रेष्ठता का दावा करते रहते हैं। निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता परिणामत: जनता में विभ्रम बना रहता है। खैर इस मुद्दे पर हम विधिवत फिर कभी लिखेंगे। भगवद्गीता में भगवान ने इस श्लोक में इस प्रकार व्रतों की ही भर्त्सना की है –
कर्षयन्त: शरीरस्थं भूतग्राममचेतस: ।
मां चैवान्त:शरीरस्थं तान्विद्ध्यवासुरनिश्चयान् ।।6।।
जो मनुष्य शरीरमें स्थित पाँच भूतोंको अर्थात् पाञ्चभौतिक शरीरको तथा अन्तःकरणमें स्थित मुझ परमात्माको भी कृश करनेवाले हैं (पीड़ित करने वाले हैं ) उन अज्ञानियोंको तू आसुर निश्चयवाले (आसुरी सम्पदावाले) समझ।
अनेक व्रतों से कामनाओं की प्राप्ति के लिए शरीर को व्रत द्वारा पीड़ित करना असुरी कृत्य है इससे अन्तर्यामी को पीड़ा पहुंचती है।
पूर्व और मध्य वैदिक काल को छोड़ दें तो उत्तर वैदिक काल में भी न इतने व्रत होते थे और न इतनी कथाएं होती थीं। हिन्दू धर्म में नित्य, नैमित्तिक और काम्य, इन भेदों से व्रत तीन प्रकार के होते हैं। जिस व्रत का आचरण सर्वदा के लिए आवश्यक है और जिसके न करने से मानव दोषी होता है वह नित्यव्रत है। सत्य बोलना, पवित्र रहना, इंद्रियों का निग्रह करना, क्रोध न करना, अश्लील भाषण न करना और परनिंदा न करना आदि नित्यव्रत हैं जिन्हें करने के लिए शास्त्रों में आदेश है। किसी प्रकार के पातक के हो जाने पर या अन्य किसी प्रकार के निमित्त के उपस्थित होने पर चांद्रायण प्रभृति जो व्रत किए जाते हैं वे नैमित्तिक व्रत हैं। ये घोर व्रत कहे गये हैं जिनका करना बहुत कठिन होता था- मसलन गो हत्या, स्त्री हत्या, बिल्ली की हत्या इत्यादि के पाप से जो पतन होता है, उससे निवृत्ति के लिए पापों का प्रायश्चित ही एकमात्र उपाय है इसलिए कठोर चांद्रायण और कृच्छ चान्द्रायण जैसे व्रत करवाए जाते थे ताकि पाप कर्म करने से मनुष्य बचे। कृच्छ चान्द्रायण का विधान कुछ इस तरह होता था-
शोधयेत् तु शरीरं स्वं पंचगव्येन मन्त्रितः।
स शिरः कृष्ण पक्षस्य तत् प्रकुर्वीत वापनम्।
शुक्ल वासाः शुचिर्भूखा मौञ्जों वन्धीत मेखलाम्
पलाश दण्डमादाय ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः।
कृ तोपवासः पूर्व तु शुक्ल प्रतिपादे द्विजः।
नदी संगम तीर्थेषु शुचौ देशे गृहेऽपिवा।
”शरीर को (दश स्नान-विधान से) शुद्ध करें। अभिमन्त्रित करके पंचगव्य पीवे। सिर को मुँड़ाकर कृष्ण पक्ष में व्रत आरम्भ करे। श्वेत वस्त्र पहने, पवित्र रहे, कटि प्रवेश में मेखला (लँगोट) धारण किये रहें। पलास की लाठी लिये रहे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। नदी के संगम, तीर्थ एवं पुष्प प्रदेशों में अथवा घर में रहकर भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में चान्द्रायण व्रत आरम्भ करें।
नदीं गत्वा विशुद्धात्मा सोमाय वरुणाय च।
आदित्याय नमस्कृत्वा ततः स्नायात् समाहितः।
उतीर्योदक माचम्य च स्थित्वा पूर्वतो मुखः।
प्राणायामं ततः कृत्वा पवित्रेरभिसेचनम्।
वीरघ्न मृषभं वापि तथा चाप्यधमर्वषम्।
गायत्री मम देवीं या सावित्रीं वा जपेत् ततः।
”शुद्ध मन से नदी में स्नान करे। सोम, वरुण और सूर्य को नमस्कार करें। पूर्व को मुख करके बैठे। आचमन, प्राणायाम, पवित्री कारण, अभिसिंचन, अधमर्षण आदि संध्या-कृत्यों को करता हुआ सावित्री-गायत्री का जप करें।”
आधारा वाज्य भागो च प्रणवं व्याहतिस्तथा।
वारुणं चैव पञ्चैव हुत्वा सर्वान् यथा क्रमम्।
प्रणम्य धाग्निं सोमं च भस्य धृत्वा यथा विधि।
“आधार होम, आज्य भाग, प्रणव, व्याहृति, वरुण आदि का विधिपूर्वक हवन करें और अग्नि तथा सोम को प्रणाम करके मस्तक पर भस्म धारण करें।”
अंगुल्थग्रे स्थितं पिण्डं गायञ्याचाभिमन्त्रयेत्।
अंगुलीभिस्त्रिभि पिण्डं प्राश्नीयात् प्रां शुचिः।
यथा च वर्धते सोमो ह्रसते च यथा पुनः।
तथा पिण्डाश्च वर्धन्ते ह्रसन्ते च दिने दिने।
”तीन अँगुलियों पर आ सके इतना अन्न का पिण्ड गायत्री से अभिमन्त्रित करके पूर्व की ओर मुख करके खाये। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा घटता है उसी प्रकार भोजन घटाये और शुक्ल पक्ष में जैसे चन्द्रमा बढ़ता है वैसे-वैसे बढ़ावे।
कृच्छ चान्द्रायण के चार भेद माने गये हैं। (1) पिपीलिका मध्य चान्द्रायण। (2) यव मध्य चान्द्रायण। (3) यति चान्द्रायण। (4) शिशु चान्द्रायण। इन चारों में 240 ग्रास भोजन ही एक महीने में करना पड़ता है। पिपीलिका मध्य चान्द्रायण वह है जिसमें पूर्णमासी का 15 ग्रास खाकर क्रमशः एक-एक ग्रास घटाते हैं और अमावस्या व प्रतिपदा को निराहार रहकर दोज से एक-एक ग्रास बढ़ाते हुए पूर्णिमा को पुनः 15 ग्रासों पर जा पहुँचते हैं।
यव मध्य चान्द्रायण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ होता है। अमावस्या के दिन उपवास करके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को एक ग्रास लेवे इसके पश्चात् पूर्णिमा तक एक-एक ग्रास बढ़ाता हुआ 15 ग्रास तक पहुँचे। इसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से एक-एक ग्रास घटाते हुए अमावस्या को निराहार की स्थिति तक जा पहुँचे।
यति चान्द्रायण में मध्याह्न को प्रतिदिन आठ-आठ ग्रास खाता रहे। न किसी दिन कम करे न अधिक।
शिशु चान्द्रायण में प्रातः 4 ग्रास और सायंकाल 4 ग्रास खाए जाते हैं और यही क्रम नित्य रहता है।
इस प्रकार इन सभी कृच्छ चान्द्रायणों में एक महीने में 240 ग्रास भोजन किया जाता है। ग्रास के दो अर्थ किये गये हैं। वीद्धायन का कथन है—
“पिण्डान् प्रकृति स्थात प्राश्नति”
साधारणतया मनुष्य जितना बड़ा ग्रास खाता है वही ग्रास का परिमाण है। महर्षि अत्रि ने इस संदर्भ में अपना मत भिन्न व्यक्त किया है। उनने लिखा है :—
कुम्कुटाण्ड प्रमाणं स्याद् यावद् वास्य मुख विशेत्।
एतं ग्रासं विजानीयुः शुद्ध्यर्थे काय शोधनम्॥
”मुर्गी के अण्डे की बराबर ग्रास माना जाय अर्थात् जितना मुँह में समा सके उसे ग्रास कहा जाय।”
ये बहुत ही कठोर व्रत होते थे जिन्हें विशेषकर ब्राह्मणों के लिए ही बनाया गया था और पातकी ब्राह्मण ही ये व्रत करते थे। वैदिक काल में पाप बहुत बड़ी चीज थी, एक छोटा से छोटा पाप कर्म भी अक्षम्य था। वर्तमान काल में किसी प्रकार के पाप कर्म से मनुष्य को भय नहीं होता।
काम्य व्रत वैदिक काल में भी प्रचलन में थे और वेदों और ब्राह्मण ग्रन्थों में बहुत से काम्य व्रतों का विधान मिलता है लेकिन तिथि आधारित व्रत नहीं मिलते। ये व्रत अनुष्ठान का हिस्सा थे, अनुष्ठान एक तपस्या है। काम्य व्रत अनुष्ठान भी होते थे जैसे पुत्रप्राप्ति के लिए राजा दिलीप ने जो गोव्रत का अनुष्ठान बारह वर्ष तक किया था। वैदिक काल में कुछ व्रत यज्ञ के यजमान करते थे मसलन जो सोमयाग का अनुष्ठान प्रारंभ करता था उसके लिए अत्यंत कठोर व्रत और नियमों का पालन करना अनिवार्य था। याग के प्रारंभ में याज्ञीय दीक्षा लेते ही उसे व्रत और नियमों के पालन करने का आदेश श्रौत सूत्र देते हैं। यागकालीन उन दिनों में सपत्नीक उस उपासक को आहार के निमित्त केवल गोदुग्ध दिया जाता था। यह भी यथेष्ट मात्रा में नहीं अपितु प्रथम दिन एक गौ के स्तन से, दूसरे दिन दो स्तनों से और तीसरे दिन तीन स्तनों से जितना भी प्राप्त हो उतना ही दूध पीने की शास्त्र आज्ञा देता है। उसी दूध का दो हिस्सा पति पत्नी को दिया जाता था। यही यजमान के लिए अहोरात्र का आहार होता था।
मनुष्य को कुछ चीजों में विशेष मोह होता है जैसे परिवार, बच्चे, पति और कुछ भय भौतिक चीजों से सम्बन्धित हैं – मसलन गरीब न हो जाएँ, रोजगार न चला जाये और धन इत्यादि की कामनाएं भी रहती ही हैं। महिलाओं को सबसे बड़ा भय दो ही रहता है -बच्चों के खोने का और पति के खोने का अथवा कोई सौतन घर में न आ जाये। पुराणों और पुराणोत्तर ज्यादातर व्रत कथाएँ इस भय के इदगिर्द ही बुनी गईं है। इस भय से लाभ कमाने का काम ब्राह्मण और साहूकार दोनों करते हैं। पुराणोत्तर व्रतकथाओं में पति की दीर्घायु की कामना के लिए किया जाने वाला करवा चौथ का व्रत कलियुग का सबसे महंगा व्रत है। साहूकार इस व्रत से एकदिन में ही बहुत धनी बन जाता है और ब्राह्मण भी लाभ कमा ही लेता है। कालान्तर में पति भी पत्नी की दीर्घायु के लिए व्रत करे इसलिए अशून्य शयन व्रत भी बनाया गया है जो चातुर्मास में हर महीने पड़ने वाले कृष्ण पक्ष की द्वितीया को पड़ता है। यह व्रत सावन महीने से आरंभ होता है और भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तक करने का विधान बनाया है लेकिन भारत एक पुरुष सत्तात्मक समाज है इसलिए पंडित न इसपर जोर देते हैं और ना ही यह किया जाता है। महिला का सबसे बड़ा मोह पुत्र में होता है इसलिए पुत्र की रक्षा के लिए अनेक व्रत हैं जो राज्यवार अलग अलग हैं। पुत्र के दीर्घायु के लिए जीवित्पुत्रिका व्रत है, अहोई अष्टमी है, छठ का व्रत ये तीन तो बहुत प्रसिद्ध हैं ही । इसके इतर भी अद्भुत संकष्ट चतुर्थी जैसे व्रत हैं जो हर महीने ही दो पक्षों में पडती है लेकिन चैत्र, सावन, भादो किसी में ज्यादा करवाते हैं। कथाओं में पुत्र के गायब होने, पति के गायब होने या मर जाने का वर्णन रहता है और कथाएं एक जैसी नहीं हैं, सब अलग अलग हैं। किसी में पृथु नामक राजा है, किसी में राजा हरिश्चन्द्र है, किसी में कोई साहूकार या ब्राह्मण है जिसका पुत्र या तो मर गया है या लापता हो गया है। ज्यादातर कथाओं में दूसरी जाति को कोई समस्या नहीं दिखती, सारे भय साहूकारों की बीबियों और राजाओं को रहता है। ब्राह्मण सनातन काल से अपनी गरीबी से भयभीत है तो उसका भय तो लाजमी ही है साथ में वह भी जरामरण में फंसा हुआ परिवार वाला ही है।
मनुष्य को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज्यादा प्रयास करना चाहिए और ईश्वर अन्तर्यामी है यह समझना चाहिए। ईश्वर से मांगने के लिए उसको कष्ट देने और पीड़ित करने की आवश्यकता नहीं है।