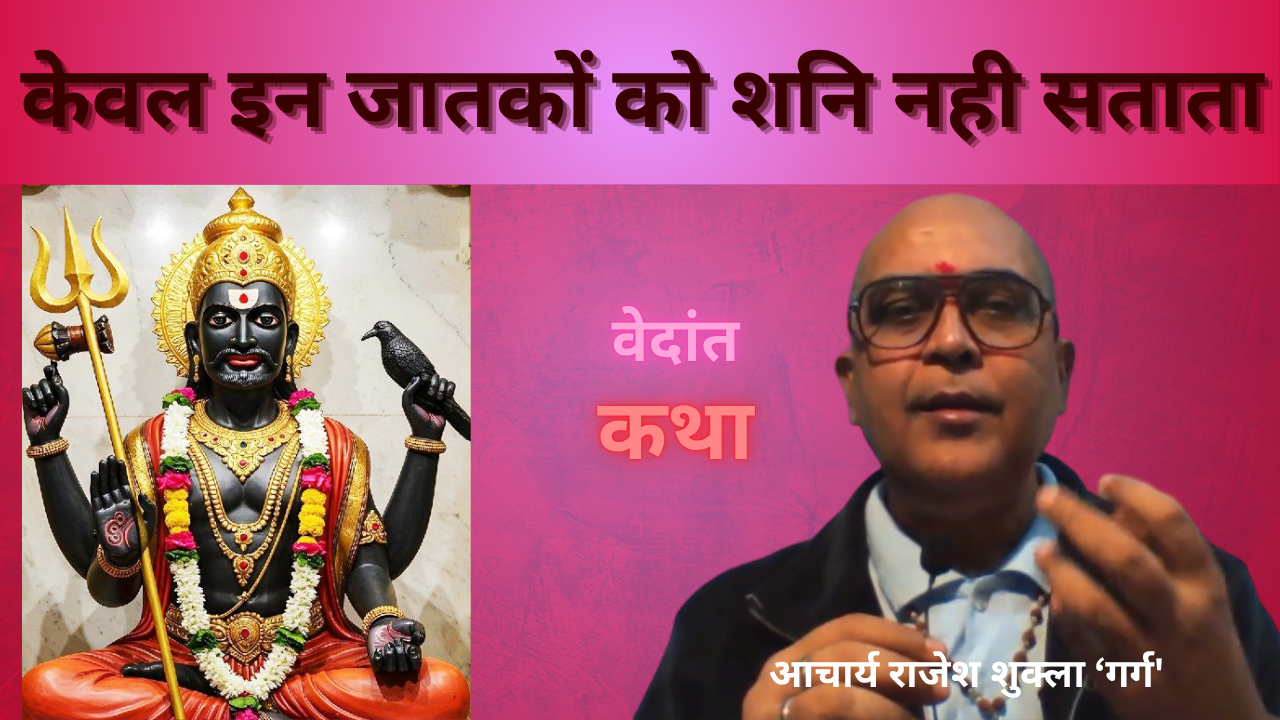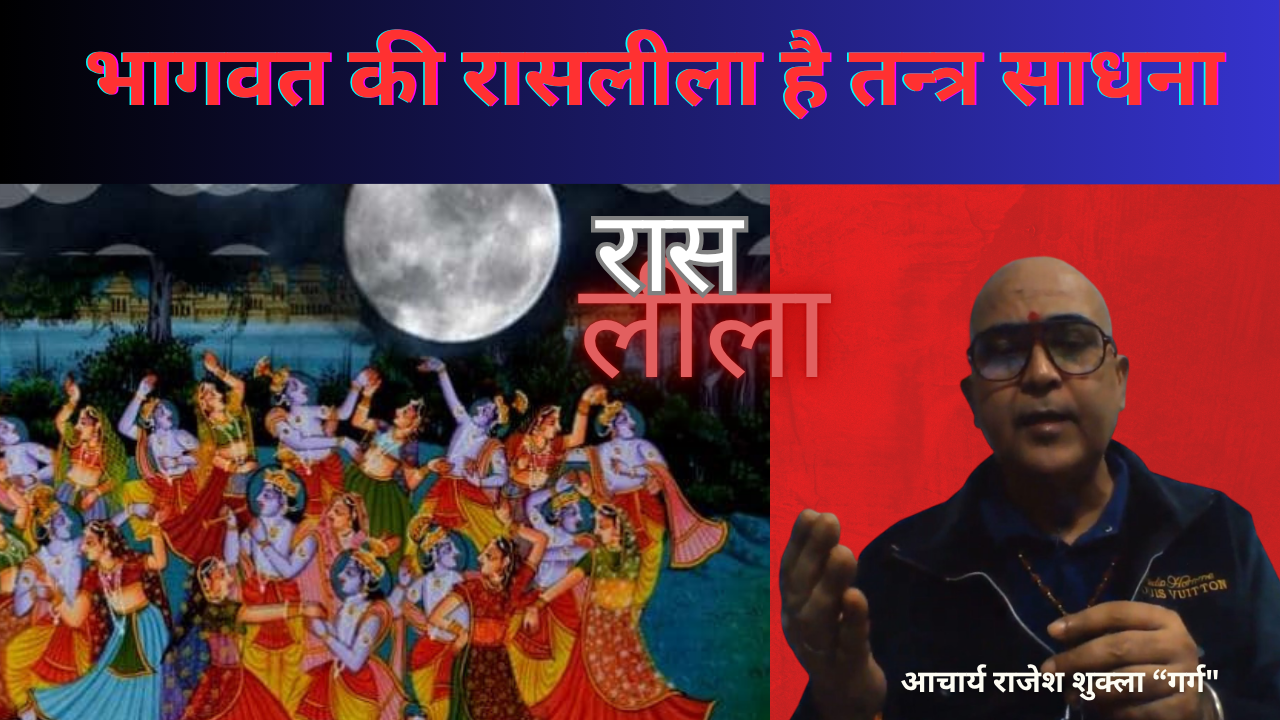यह उपदेश थोड़ा प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले बाबा का उपदेश है इसलिए इसमें देवताओं पर कटाक्ष है “काली जीभ निकाल कर चिढाती है ?” “देवी बाल खाती हैं ?” इत्यादि, लेकिन आचार्य का उपदेश को यदि ठीक से समझेंगे तो उसका निहतार्थ आवश्य समझ में आ जायेगा. पाठक इससे यह न समझे कि श्री राम शर्मा आचार्य का तात्पर्य कटाक्ष है या श्रद्धालुओं का उपहास उडाना है. यह उनके लिए कहा गया है जो मन्दिर जाते हैं लेकिन स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करते. उनमे सारे दुर्गुण रहते हैं बल्कि मन्दिर में जाकर वापस आते हैं तो ज्यादा पाप करते हैं. ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें यह ज्ञान नहीं कि देवता वास्तव में उदात्त भाव हैं, जो कुछ भी जीवन में श्रेष्ठ है उसमे देवता का निवास होता है जैसे सत्य, अचौर्य, अहिंसा, अपरिग्रह इत्यादि.
क्या होते हैं देवी- देवता
देवत्व का अर्थ होता है- श्रेष्ठताएँ। देवता कहाँ रहते हैं? हमें नहीं मालूम। हम एक बार कैलाश पर्वत पर थे तो मरते-मरते बचे थे। देवता कहाँ रहते हैं? पीपल के पेड़ पर रहते होंगे। अच्छा तो चलिए दिखाइए। नहीं साहब! वहाँ तो देवी रहती है। कहाँ रहती है? महाराज जी! वह तो नगरकोट में रहती है, कलकत्ता (कोलकाता) में रहती है। अच्छा तो वहीं चलो। मैं तो कलकत्ता देख आया हूँ। वहाँ काली जीभ निकालकर चिढ़ा रही है। किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि क्यों साहब! काली देवी जीभ निकालकर क्यों चिढ़ाती है? अरे भाई! जीभ निकालना उनका शौक है। महाराज जी! एक देवी नगरकोट में रहती हैं। मेरे बाल-बच्चों का मुंडन वहाँ होगा। अच्छा बेटे! तेरी कुलदेवी कहाँ रहती है। महाराज जी! बाड़मेर में, जैसलमेर में। तो वहाँ क्या करेगा? बच्चे का मुंडन कराऊँगा। और कहीं करा ले तो? नहीं महाराज जी! देवी नाराज हो जाती है। क्या कहती है तेरी देवी? यों कहती है कि मैं बाल खाऊँगी, तू बाल यहीं काट। बेटे तू ऐसा भी कर सकता है कि घर पर मुंडन करा ले और बाल एक डिब्बे में बंद करके उसे देवी के पास पार्सल से भेज दे, देवी के काम आएगा। नहीं महाराज जी! देवी कहती है कि मुंडन के लिए हमारे यहाँ ही आना पड़ेगा, नहीं तो वह नाराज हो जाएगी।
साथियो! आपने देवी देखी है क्या? अगर देखी हो तो मुझे भी बता देना। मैंने तो देखी नहीं ऐसी देवी जो मुंडन कराती हो और बाल खाती हो। मैंने जो देवी देखी है, वह विचारणाओं के रूप में, भावनाओं के रूप में, सिद्धांतों के रूप में देखी है। मनोवृत्तियों के रूप में और कृतियों के रूप में देवियाँ देखी हैं। इनमें से एक का नाम दया की देवी, एक का नाम करूणा की देवी, एक का नाम श्रद्धा की देवी, एक का नाम दान की देवी है। मैंने असंख्य देवियों की पूजा की है और उनके साथ में इतना आनंद उठाया है कि वे मेरी सहेलियों की तरह, मित्रों की तरह मुझे हँसाती रहती हैं, मुझे खिलाती रहती हैं। देवियों के उघान में मैं विचरता रहता हूँ और देवियाँ मुझे प्यार देती रहती हैं। मरने के बाद स्वर्ग में जिन देवियों और अप्सराओं का वर्णन किया गया है,उन देवियों और अप्सराओं को मैंने इसी वन में देखा है, प्रकृति के रूप में और प्रवृत्तियों के रूप में।
मित्रों! देवता कर्म हो सकता है, देवता विचार हो सकता है, देवता भावना हो सकता है, देवता व्यक्ति नहीं हो सकता। देवता अगर व्यक्ति होता तो दुनिया में छाया रहता, एक जगह नहीं रहता। शंकर जी शैवों में छाए रहते हैं। देवी शाक्तों में छाई रहती है और विष्णु भगवान वैष्णवों में छाए रहते हैं और रामचंद्र जी राम भक्तों में छाए रहते हैं, खुदाबंद करीम मुसलमानों में छाए रहते हैं। बेटे! इतने सारे भगवान नहीं हो सकते। सारी दुनिया में एक ही तरह का भगवान हो सकता है, अनेक तरह का कैसे हो सकता है? तो क्या अनेक तरह के भगवान नहीं हो सकते? बेटे! हमें विश्वास नहीं कि अनेक तरह के भगवान होते हैं। हमारा विश्वास इस बात के ऊपर है कि भगवान की जो असंख्य शक्तियाँ हैं, वे मनुष्य के भीतर जब प्रवेश करती हैं तो वे देववृत्तियों के रूप में प्रवेश करती हैं।
देववृत्तियाँ जहाँ हैं, वहाँ हैं देवता
देववृत्तियाँ किसे कहते हैं? श्रेष्ठ चिंतन एक, श्रेष्ठ कर्म दो, श्रेष्ठ भावनाएँ तीन- इन्हीं का नाम देववृत्तियाँ हैं। वे श्रेष्ठताएँ जिनमें होगी, उन्हें अगर मैं देवता कहूँ तो आप बुरा मत मानना। वास्तव में यही देवता हैं। बाहर के प्रतीको के माध्यम से जनसाधारण को हम सिखाते हैं कि ये प्रतीक वास्तव में हमारे देवता हैं। प्रतीक हाँ बेटे प्रतीक। शंकर जी की जब हम पूजा करते हैं, तो हम कुछ प्रतीक के माध्यम से उन संवेदनाओं की, सिद्धांतों की, आदर्शो की पूजा करते हैं, जो शंकर जी में समाविष्ट हैं। जैसे कि शंकर जी के सिर में से ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है। शंकर जी के मस्तक पर संतुलन का चंद्रमा टिका हुआ है। जिन्होंने मुंडों कि माला अर्थात मृत्यु को संगिनी बनाने के लिए अपने गले में मुंडों की माला पहनी हुई है। जिन्होंने साँपों को गले से लगाकर रखा है। जिसका कि तीसरा नेत्र खुला हुआ है। तीसरा नेत्र कोन सा? विवेक का नेत्र, ज्ञान का नेत्र, देवता का नेत्र, आज से लेकर हजारों वर्षों तक आगे और पीछे की अपनी परिस्थितियों को देख सकने वाला ‘टेलिस्कोप’ जिससे कि हम भविष्य देखते हैं। जिससे हम अपने बुढ़ापे को देखते हैं, जिससे अपनी मृत्यु को देखते हैं, जिससे हम परलोक को देखते हैं, जिससे हम जन्म-जन्मांतरों को देखते हैं, ऐसा हमारा टेलिस्कोप ‘तृतीय नेत्र’ खत्म हो गया है।
मित्रों! आज हमको अनीति दिखाई पड़ती है। साठ साल की उम्र में क्या कर रहा है? गुरूजी! हमारे तो साढ़े सात नंबर का चश्मा चढ़ गया है और वह खो गया है। तो अब आपको दिखाई नहीं पड़ता? हाँ गुरूजी! हमें दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा तो अभी के फायदे के पीछे आप अपने भविष्य का सत्यानाश करने पर उतारू हैं। भविष्य को देखिए, बुढ़ापे को देखिए, परलोक को देखिए, मृत्यु को देखिए और जन्म-जन्मांतर को देखिए। क्या आगे वाली चीजें नहीं देख सकते? नहीं साहब! हमको दिखाई नहीं पड़तीं। तो आप शंकर जी की भक्ति कीजिए और उनसे वरदान माँगिए कि आपने जो अपना विवेक का तीसरा नेत्र खोला हुआ था, वह हमारा भी खोल दीजिए।
मस्तिष्क का संतुलन किसे कहते हैं? जिसमें आदमी ऐसे भी और वैसे भी अर्थात दोनों परिस्थितियों में ‘बैलेंस’ कायम रख सकता है। साइकिल सवार को अपना ‘बैलेंस’ कायम रखना पड़ता है। बैलेंस गँवा देगा तो इधर गिरेगा या उधर गिरेगा और हाथ-पैर तुड़वा बैठेगा। अतः साईकिल चलाते समय बैलेंस बनाकर चलते हैं। किसी भी कार्य में अगर हम संतुलन कायम नहीं रख सकते, तो सफलता नहीं मिल सकती। यहाँ तक की हम खुशी में भी संतुलन नहीं कायम रख पाते तो हम पागल हो जाते हैं और व्यसन तथा व्यभिचार कि ओर मुड़ जाते हैं। जब हम गरीब होते हैं तो चोरी करने पर विवश हो जाते हैं। हमारा ‘बैलेंस’ यों भी खराब हो जाता है और यों भी खराब हो जाता है।
मित्रों! ‘ बैलेंस’ रखने वाली बत्ती का नाम है- मस्तिष्क। मस्तिष्क पर चंद्रमा होने का मतलब है-ज्ञान की गंगा, अमृत की धारा का प्रवाहित होना। ज्ञान की धाराएँ, अमृत की धाराएँ प्रवाहित होते रहने से मतलब है, हमारा मस्तिष्क स्वंय ज्ञान से भरा रहे और अपने श्रेष्ठ विचारों से सारे समाज में ज्ञान की गंगा बहाते चलें।
शंकर भगवान भूत-प्रेतों के साथ प्रेम करने वाले हैं। भूत-प्रेतों के हाल सुधारने के लिए खड़े होने वाले, पापी एवं पतित लोगों को सहारा देने वाले, ऊँचा ऊँठाने वाले ही सच्चे अर्थों में शिवभक्त कहे जा सकते हैं। बाबा आम्टे की तरह से जिन्होंने कोढ़ियों का विघालय शुरू किया और अब वहाँ नागपुर के पास उनका विश्वविघालय भी बन चुका है। अभी-अभी अखबार में छपा है, उनकी फोटो भी छपी है, जिसकी कटिंग भी मैंने रखी है। टी.वी पर भी देखा है। उन्होंने सारी जिंदगी पीड़ितों के लिए, पतितों के लिए, कोढ़ियों के लिए खरच कर दी। अंधों के लिए, गूँगों के लिए, बहरों के लिए उन्होंने एक आश्रम बनाया, जहाँ उनका प्रशिक्षण होता है और उनमें से समाजसेवी निकलकर बाहर आते हैं। ऐसा है उनका विश्वविघालय। ये हमारी वो वृत्ति है, जिसका ज्ञान की गंगा के रूप में प्रवाहित होना स्वभाव है। ये वृत्तियाँ देववृत्तियों के रूप में, देवताओं के रूप में हमारे भीतर विघमान हैं। उन्हें विकसित करने के लिए, उभारने के लिए ही देवपूजन की पंचोपचार प्रक्रिया अपनाई जाती है।
देवपूजा का तत्त्वज्ञान
भारतीय संस्कृति देवपूजा में विश्वास करती है। ‘देव’ शब्द का स्थूल अर्थ है- ‘देने वाला’, ज्ञानी, विद्वान आदि श्रेष्ठ व्यक्ति। देवता हमसे दूर नहीं हैं, वरन पास ही हैं। हिंदू धर्मग्रंथों में जिन तैंतीस करोड़ देवताओं का वर्णन किया गया है, वे वास्तव में देव- शक्तियाँ हैं। ये ही गुप्त रूप से संसार में नाना प्रकार के परिवर्तन, उपद्रव, उत्कर्ष उत्पन्न करती रहती हैं।
हमारे यहाँ कहा गया है कि देवता ३३ प्रकार के हैं, पितर आठ प्रकार के हैं, असुर ९९ प्रकार के, गंधर्व २७ प्रकार के, पवन ४६ प्रकार के बताए गए हैं। इन भिन्न- भिन्न शक्तिओं को देखने से विदित होता है कि भारतवासियों को सूक्ष्म विज्ञान की कितनी अच्छी जानकारी थी और वे उनसे लाभ उठाकर प्रकृति के स्वामी बने हुए थे। कहा जाता है कि रावण के यहाँ देवता कैद रहते थे, उसने देवों को जीत लिया था।
हिन्दुओं के जो इतने अधिक देवता हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने मानवता के चरम विकास में असंख्य दैवी गुणों के विकास पर गंभीरता से विचार किया था। प्रत्येक देवता एक गुण का ही मूर्त रूप है। देवपूजा एक प्रकार से सद्गुणों, उत्तम सामर्थ्यों और उन्नति के गुप्त तत्त्वों की पूजा है। जीवन में धारण करने योग्य उत्तमोत्तम सद्गुणों को देवता का रूप देकर समाज का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया गया। गुणों को मूर्त स्वरूप प्रदान कर भिन्न भिन्न देवताओं का निर्माण हुआ है। इस सरल प्रतीक पद्धति से जनता को अपने जीवन को ऊँचाई की और ले जाने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ।
आप चाहे जिस हिंदू देवी- देवता की पूजा- आराधना करें, वह उसी जगत नियंता की एक शक्ति का रूप है। यह देवत्व का एक पहलू है जो आपके व्यक्तित्व में विकसित होकर आपको सामर्थ्यवान बना सकता है।
आरोग्यं भास्करादिच्छेत्
धनामिच्छेदधुताशनात्।
ज्ञान च शंकरादिच्छेत्
मुक्तिमिच्छेत जनार्दनात् ।।
आरोग्य की कामना सूर्यनारायण से करें, धन की इच्छा हुताशन (अग्निहोत्र) से पूरी करें। ज्ञान के लिए शंकर जी की आराधना करें और मुक्ति के लिए जनार्दन का आश्रय ग्रहण करें।
इस श्लोक का स्थूल अर्थ तो यही है कि अमुक- अमुक अभिलाषा के लिए अमुक- अमुक देवता की पूजा, आराधना, चिंतन इत्यादि करें। पूजा- अर्चा का साधारण अर्थ हम लोग गंध, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, तांबूल, अर्घ, स्तोत्र, नमस्कार आदि ही समझते हैं और इतना कर्मकाण्ड कर लेने मात्र से यह आशा करते हैं कि देवता लोग प्रसन्न होकर हमें मनोवाँछित वस्तुएँ प्रदान कर देंगे। परंतु हम देखते हैं कि अनेक मनुष्य इस प्रकार की ऊपरी पूजा अर्चाओं में बहुत समय तक लगे रहते हैं, तो भी उनकी इच्छाएँ पूर्ण नहीं होती हैं। ऐसी दशा में उपर्युक्त शास्त्रवचन की सत्यता पर संदेह सा होने लगता है।
गंभीर दृष्टि से देखा जाए, तो हम वचन में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। असफलता का कारण हमारा एकांगी दृष्टिकोण है।
हम समझते हैं कि हिंदू देवताओं को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक कर्मकाण्ड की पूजा पत्री ही पर्याप्त है, पर वास्तविक बात ऐसी नहीं है, हिन्दू देवी देवताओं का वास्तविक रूप समझना चाहिए। प्रत्येक देवी देवता का एक व्यावहारिक रूप है जो हमारे दैनिक जीवन में कर्म पर निर्भर है। ये देवता हमसे यह माँग करते हैं कि हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम जगत में ठोस कर्म करें, उनके द्वारा दिखाई हुई दिशा में परिश्रम करें, अपने उद्देश्य में तन्मय हो जाएँ, संक्षेप में अपने मन, वचन से इनमें अपने को नियोजित कर दें, तभी सच्ची पूजा संभव हो सकती है। कर्म से प्रसन्न होकर ही ये देवता मनोवाँछित फल दिया करते हैं। ये कार्य शक्तियों के प्रतीक हैं। जब हम किसी मनोवाँछित देवता को चुनें तो हमें उसके व्यावहारिक मनोरूप को अवश्य समझ लेना चाहिए।
उदाहरण के लिए सूर्य देवता से हम आरोग्य, बल, स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन की कामना करें। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि हम सूर्य की किरणों, प्रकाश, वायु, खुला जीवन से घनिष्ठता रखें। शरीर को प्रकृति के सहयोग में आने दे। प्राकृतिक जीवन जिएँ। बदन को कपड़ों से ऐसा न लपेट लें कि त्वचा तक प्रकाश और वायु ही न पहुँच सके। सूर्य को ‘नारायण’ विशेषण दिया गया है, जिसका गुप्त तात्पर्य यह है कि उसकी किरणों में जीवनदायी शक्तियाँ हैं। ये रोग के कीटाणुओं को मारने की प्रचंड शक्ति रखती हैं, जितनी किसी बहुमूल्य दवाई में भी नहीं मिल सकती। जो व्यक्ति प्रकृति से निकट संपर्क रखते हैं और खुली धूप, वायु, प्रकाश आदि में कार्य करते हैं, वे दीर्घजीवी और नीरोग रहते हैं। कहा भी है- ”जहाँ धूप और हवा नहीं पहुँचती, वहीं डॉक्टर पहुँचते हैं।” प्रकृति के फल−फूल, जीवों की देखिए। फल, वनस्पति, वृक्ष आदि का जो भाग धूप से सीधा संबंध रखता हैं, वहाँ प्राणशक्ति अधिक पाई जाती है। फलों के, शाक- भाजियों के, अन्नों के छिलके सूर्य- किरणों के सीधे संपर्क में आते है। इसलिए भीतरी भाग की अपेक्षा उनके छिलकों में पोषक तत्त्व (विटामिन) अधिक पाए जाते हैं। सूर्य- स्नान, सूर्य किरण चिकित्सा, सूर्य- नमस्कार, सूर्य- सेवन, सूर्य उपासना, सूर्य- माहात्म्य आदि सभी का चिकित्सा पद्धतियों और वैद्यक में बड़ा महत्त्व माना गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य के इन असंख्य लाभों को देखकर ही हिंदू तत्त्वज्ञानियों ने सूर्य को ‘नारायण’ का दिव्य विशेषण प्रदान किया है। सूर्य शक्ति को जीवन में अधिक से अधिक व्यवहार करना यही सूर्य- पूजा है, जिससे आरोग्य की वृद्धि होती है।
हुताशन- अग्निहोत्र का वास्तविक अर्थ है- ‘साहसपूर्ण त्याग’। अग्निहोत्र में पहले हम अपनी मूल्यवान हवन- सामग्री श्रद्धापूर्वक हवन करते हैं, तब उस यज्ञ का फल मिलता है। जो व्यक्ति कठिन श्रम, जिम्मेदारी, ईमानदारी तथा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं, वे ही धन कमा पाते हैं। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले, आलसी, साहसहीन व्यक्ति कोई ऊँचा काम नहीं कर सकते और न धन कमा सकते हैं। किसान अपना अन्न खेत में बिखेर देता है, धैर्यपूर्वक छह महीने खेत को अपने पसीने से सींचता रहता है, एक बीज के बदले सौ चीज उसे मिलते हैं। साहसी पुरुषों के गले में लक्ष्मी की जयमाला पड़ते देखी जाती है। धैर्यवान, अग्नि तप सा कठोर परिश्रम करने वाले, अपने कारोबार पर एकाग्रचित्त से श्रद्धा रखने वाले लोग सफलता प्राप्त करते हैं। यही अग्नि- पूजा का वास्तविक व्यवहारिक स्वरूप है। जो व्यक्ति अग्निदेवता की पूजा का विधान समझता है, उसे अग्नि जैसा कठोर तप करना चाहिए।
ज्ञान के लिए शंकर भगवान की आराधना का विधान है। शिवशंकर संयमी, निस्पृह, त्यागी, योगस्थित (एकाग्रचित्त), उदारमना हैं। शंकर जी के इन गुणों को अपने चरित्र तथा दैनिक कार्यों में प्रकट करने वाले व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में ज्ञानवान बनते हैं। उन्हें तत्त्वदर्शन प्राप्त होता है। असंयमी, ममताग्रस्त, लोभी, डाँवाडोल चित्त वाले, अनुदार वृत्तियों वाले लोग शिक्षा की उत्तम व्यवस्था होने पर भी अधूरा और उलटा ज्ञान ही प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान नहीं, एक प्रकार का अज्ञान है, जिससे उनमें असत्य, छल, अपहरण, शोषण, अहंकार, असंयम जैसे दुर्गुणों की वृद्धि होती है। जिनमें शंकर तत्त्व की स्थिति मौजूद है, वे कोई गुरु न होते हुए भी एकलव्य की तरह मिट्टी की मूर्ति को गुरु बना लेते हैं, कबीर की तरह गुरु की बिना जानकारी मेंही दीक्षा ले लेते हैं। दत्तात्रेय को तरह मकड़ी, मक्खी, कौवे, कुत्ते जैसे निम्न कोटि के जीवों को गुरु बनाकर उनसे अपना ज्ञान- भंडार भर लेते हैं। ज्ञानप्राप्ति के लिए अपने अंदर शंकर- तत्त्व की स्थापना आवश्यक है। इसका यही व्यवहारिक रूप है।
मुक्ति के लिए जनार्दन की पूजा की जाती है। जनता- जनार्दन की पूजा को, लोकसेवा को, अनेक तत्त्वदर्शियों ने मुक्ति का साधन माना है। प्राणिमात्र में समाए हुए सजीव भगवान की पूजा करना कितने ही महर्षियों वे निर्जीव प्रतिमा पूजा की अपेक्षा कहीं ऊँचा माना है। इस प्रकार लोकसेवा, ईश्वर- पूजा ही ठहरती है, उससे मुक्ति का द्वार खुल जाता है।
हिंदू देव- पूजा प्रत्यक्ष फलदायी साधना है। हिंदू अपने चारों ओर प्रत्येक जीव, वृक्ष, पशु मनुष्य सबमें भगवान को ही व्यापक देखता है। संसार के सब प्राणियों और अपने आस- पास के मनुष्यों को जनार्दनमय समझता है। ऐसा व्यक्ति गुप्त या प्रकट रूप से किसी के प्रति कोई बुराई नहीं कर सकता। ऐसा सात्त्विक आचार और विचार वाला व्यक्ति अपने सतोगुण के कारण दूसरों को मुक्त करता और स्वयं जीवनमुक्त हो जाता है।
हमारी देवपूजा में इसी प्रकार के गुप्त अभिप्राय कूट- कूटकर भरे हुए हैं। ये हमारे अंदर छिपे हुए पौरुष एवं पराक्रम को जाग्रत करने के प्रतीक हैं। ये गुणों की स्थूल प्रतिमाएँ हैं। आज अज्ञानवश हिंदू अपनी इन छिपी हुई शक्तियों को भूल गए हैं, अन्यथा इनमें ज्ञान, अध्यात्म, धर्म, विवेक, रसायन का अतुलित ज्ञान भंडार भरा हुआ है।