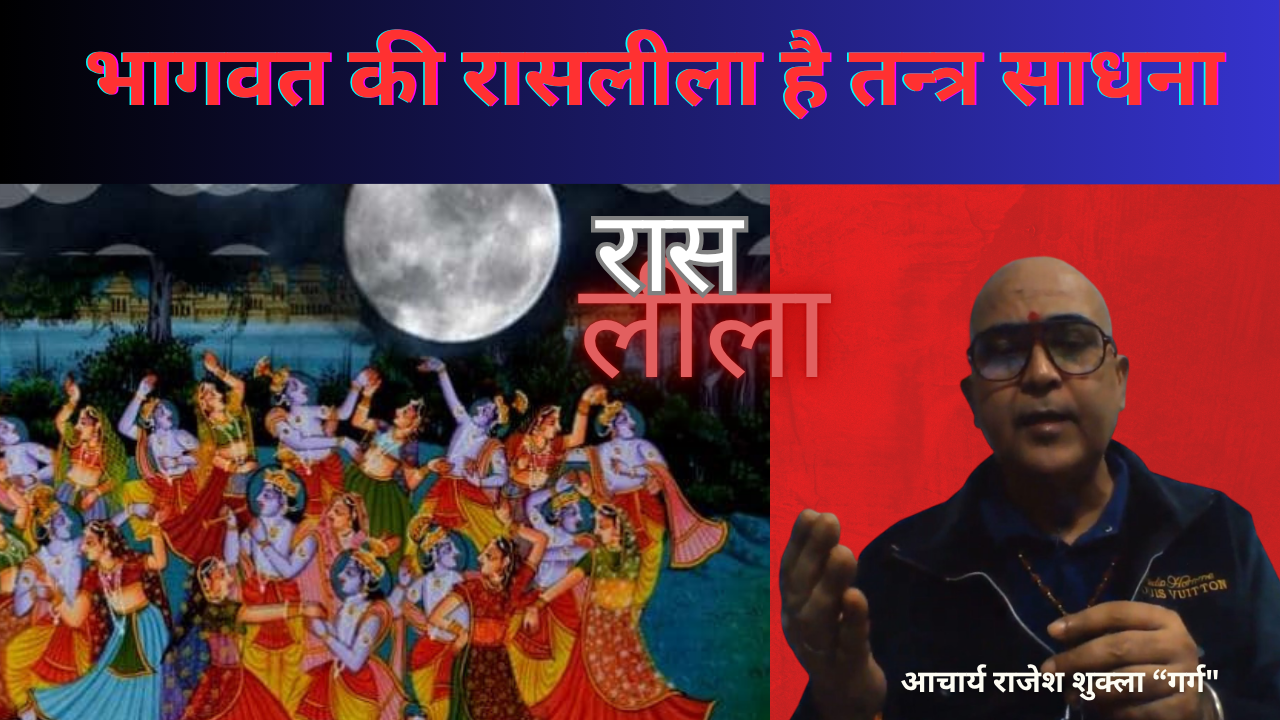वैदिक वांग्मय में उपनिषदों का स्थान सबसे ऊपर है। कहा भी है- ‘चतुर्णांमपि वेदानां उपनिषद: शिर:’ चारो वेदों का उपनिषद ही सिर हैं। उपनिषद को ही वेदांत कहा गया है क्योंकि ये वेदों का अंत भाग हैं। उपनिषदें 108 की संख्या से भी ज्यादा उपलब्ध हैं। कुछ विद्वानों ने दो सौ से ज्यादा उपनिषदें संकलित की हैं जिनमें अनेक उपनिषदें विगत 2000 साल के भीतर लिखी गईं हैं। प्रमुख उपनिषद 12 हैं- जिनमे ईश, ऐतरेय , कठ , केन , छान्दोग्य , प्रश्न, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक ,मांडूक्य, मुण्डक, कौषीतकी और मैत्रायणी उपनिषद हैं। इनमें कौषीतकी और मैत्रायणी को छोड़ कर शेष दस उपनिषदों पर भगवान आदि शंकर ने भाष्य किया है। आदि शंकराचार्य उपनिषदों, भगवद्गीता और ब्रह्मसूत्र के पहले भाष्यकार हैं इसलिए उनके दिए साक्ष्य और तर्क उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने श्रुतियों के प्रमाण।
कौषीतकी तथा मैत्रायणी भी महत्वपूर्ण उपनिषद मानी गई हैं जिनका भगवान शंकराचार्य ने भाष्यों में प्रमाण के रूप में उद्धरण दिया है। अनेक छोटी उपनिषदों में आचार और साधन प्रधान है तथा अनेक उपनिषदें देवी दवताओं और पन्थ विशेष से सम्बन्धित हैं। इन्हें गौड़ श्रेणी में रखा गया है। सभी उपनिषदों का विषय ब्रह्मविद्या ही है भले ही कोई उपनिषद किसी देवता या पन्थ से ही सम्बन्धित क्यों न हो। उपनिषद संसार बंधन का कारण अर्थात अविद्या की आत्यंतिक निवृत्ति के साधन के रूप में रचे गये। भगवान आदि शंकराचार्य ने उपनिषद का अर्थ करते हुए लिखा है –‘सेयं ब्रह्मविद्या उपनिषच्छब्दवाच्या तत्पराणां सहेतो: संसारस्यात्यन्तावसादनात् । तादर्थ्याद् ग्रंथोऽप्युपनिषद् उच्यते’ यह ब्रह्मविद्या अपने में लगे हुए पुरुषों के संसार का कारण सहित अत्यंत अवसान (उच्छेद ) करती है, इसलिए उपनिषद शब्द से कही जाती है क्योंकि ‘उप’ और ‘नि; उपसर्ग पूर्वक सद् धातु का यही (अवसादन ही) अर्थ है ।
उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति रूप प्रयोजन वाला होने के कारण ये ग्रन्थ उपनिषद कहे जाते हैं। उपनिषद वेदों के कर्मकांड भाग के अंत में लिखे गये हैं अर्थात उपनिषद का प्रारम्भ तभी होता है जब व्यक्ति को संसार में कोई रस नहीं रहता, विषयों से उसका चित्त व्यग्र हो उठता है; उसे दुनिया में कोई चीज आकृष्ट नहीं करती । इस दुःख और बंधन का कारण क्या है ? इस जिज्ञासा के साथ वह गुरु के पास जाता है, उपवेशन करता है और उनसे अपनी जिज्ञासा से सम्बन्धित प्रश्न पूछता है। यह शास्त्र ब्रह्म जिज्ञासा से प्रारम्भ होता है इसलिए इसे उपनिषद कहते हैं। अन्य प्रकार से कहें तो ‘उप सामीप्येन निनितरां, प्राप्नुवन्ति परं ब्रह्म यया विद्यया सा उपनिषद’ जिस विद्या के द्वारा पर ब्रह्म का सामीप्य एवं तादात्म्य प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं।
भगवान ने भगवद्गीता में भी उपनिषद का अर्थ निर्देशित किया है –
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया।
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः।
अर्जुन को उपदेश में भगवान ने कहा – अर्जुन ! ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठतम है क्योंकि सभी कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं ‘सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते’। अब वह ज्ञान जिस विधिसे प्राप्त होता है वह तू सुन। आचार्यके समीप जाकर भलीभाँति दण्डवत् प्रणाम करने से एवं किस तरह यह संसार बन्धन हुआ? कैसे मुक्ति होगी? विद्या क्या है? अविद्या क्या है इस प्रकार ( निष्कपट भावसे ) प्रश्न करने से और गुरु की यथायोग्य सेवा करनेसे ( वह ज्ञान प्राप्त होता है )। अभिप्राय यह कि इस प्रकार सेवा और विनय आदि से प्रसन्न हुए तत्त्वदर्शी ज्ञानी आचार्य तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे। ज्ञानवान् भी कोई कोई ही यथार्थ तत्त्व को जानने वाले होते हैं सब नहीं होते। इसलिये ज्ञानी के साथ भगवान ने तत्त्वदर्शी यह विशेषण भी लगाया है ।
उपनिषद तत्वदर्शी ऋषियों द्वारा प्रदत्त ब्रह्म विद्या है।
भारत के उदात्त तत्व दर्शन और धर्म सिद्धांतों का मूल आधार ये उपनिषद ही हैं जिसे भगवान बादरायण ने ब्रह्म सूत्र में ‘शास्त्रयोनित्वात’ सूत्र से अभिव्यक्त किया है। प्रस्तुत ‘आत्मपूजोपनिषद’ निवृत्ति मार्ग की बहुत छोटी उपनिषद है और सूत्रों में लिखी गई है। जैसा की नाम से ही अस्पष्ट है इस उपनिषद का विषय आत्मपूजा है। आत्मपूजा अन्तर्याग की तरह ही है जिसमें किसी पंचतत्वात्मक पूजन सामग्री की जरूरत नहीं होती, भावना ही प्रमुख द्रव्य होता है। फूल माला इत्यादि से पूजन कोई वास्तविक पूजन नहीं है, यह सामरस्य नहीं करता । निर्विकल्प महाव्योम में लीन होना और संविद साक्षात्कार करना ही वास्तविक पूजा है। उपनिषद कहती है कि जब आत्मा के इतर कोई और है नहीं तो ध्यान का विषय भी यह आत्मा ही है। आत्मतत्व का निरंतर चिन्तन ही ध्यान है। आत्मतत्व के चिन्तन में जब साधक का अस्तित्व सरोबार हो जाता है तब उसका उठाना बैठना, उसका हाव भाव सब मुद्रा हो जाते हैं। आत्मस्वरूप में समावेश होने पर ये सिद्ध लकड़ी और औषधियों का धुआं नहीं फैलाते, ये ‘विश्वं जुहोमि स्वाहा’ बोल कर विश्वमेध में हवन की क्रीड़ा करते हैं। विद्याओं की साधना के अंत में साधक यही तो बोल पड़ता है –
आर्द्रं॒॑ ज्वल॑ति॒ज्योति॑र॒हम॑स्मि । ज्योति॒र्ज्वल॑ति॒ ब्रह्मा॒हमस्मि ।
यो॑ऽहम॑स्मि॒ ब्रह्मा॒हम॑स्मि । अ॒हम॑स्मि॒ ब्रह्मा॒हम॑स्मि । अ॒हमे॒वाहं मां जु॑होमि॒ स्वाहा᳚ ॥
शास्त्रों के अनुसार कलियुग में चार गुना जप से मन्त्र की सिद्धि होती है इसलिए मन्त्र स्वरूप उपनिषदों की व्याख्या में चार गुना प्रयास करना चाहिए।
यह लेख आचार्य राजेश शुक्ला गर्ग के भाष्य आत्मपूजा उपनिषद से लिया गया है
ATMAPUJA UPANISHAD: आत्मपूजोपनिषद (Hindi Edition)
किंडल संस्करण